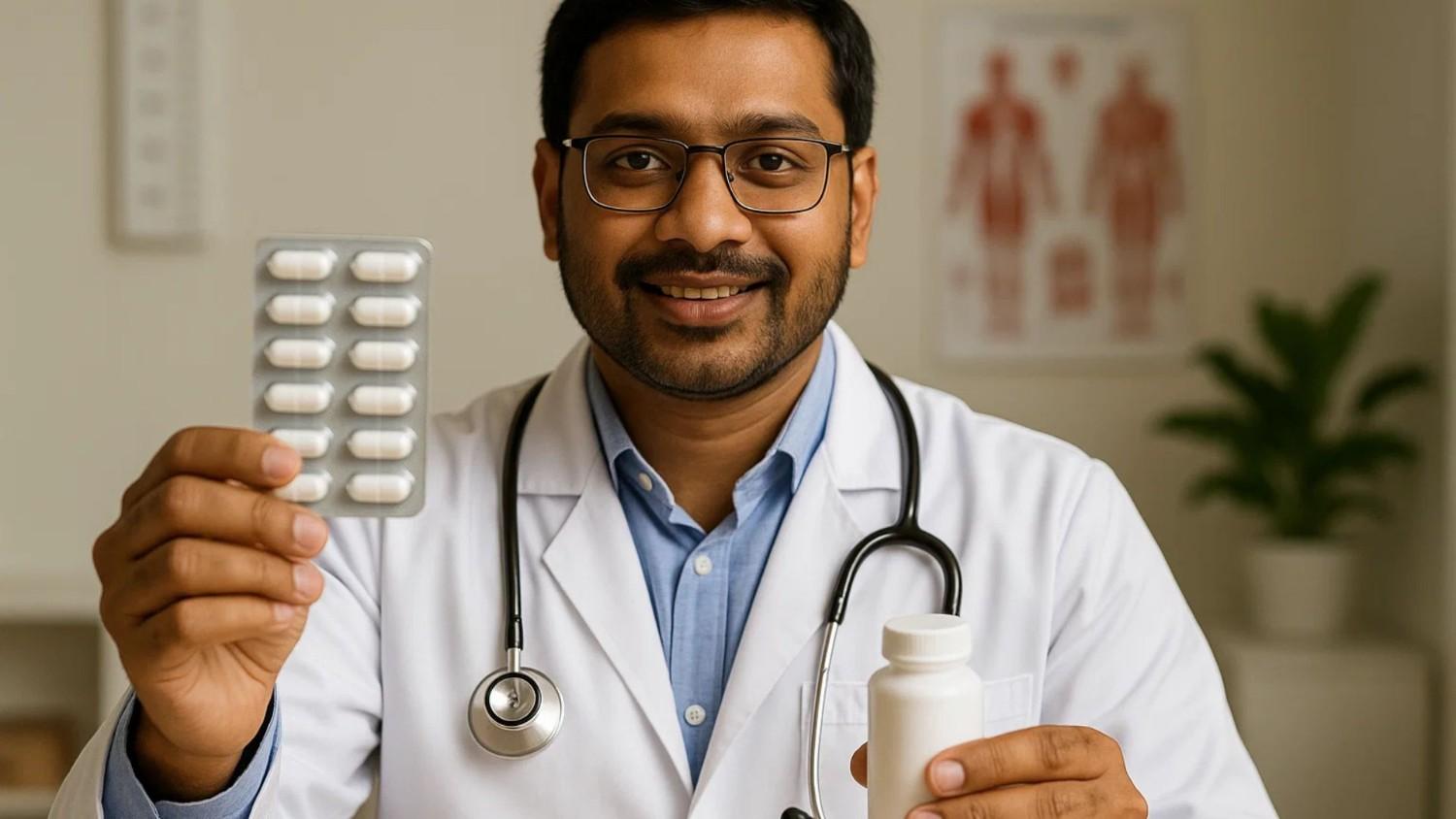पिछले दिनों मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब पंजाब ने भी इसको राज्य में बैन कर दिया है। एमपी में अब तक 17 बच्चों की मौत हो गई है। देश के कई और राज्य इस दवा को लेकर हरकत में आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये दवाएं खास तौर पर बच्चों के सिरप बाजार या मरीज तक आने का क्या प्रोसेस है?
मध्य प्रदेश में खासकर छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में जहरीले कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। अकेले छिंदवाड़ा में 15 बच्चों की मौत हुई है। अधिकांश बच्चों की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई। तमिलनाडु की लैब रिपोर्ट में 'कोल्ड्रिफ' (Coldrif) नाम की इस कफ सिरप के एक बैच में डायएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक जहरीला केमिकल बड़ी मात्रा में पाया जो किडनी के लिए खतरनाक है। इसके बाद एमपी सरकार ने तमिलनाडु की दवा कंपनी एसरेसन फार्मास्यूटिकल्स के सभी उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया।
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में चला बुलडोजर, भारी पुलिसबल तैनात; तनाव का माहौल
कई बच्चों को यह सिरप प्रिस्क्राइब करने वाले स्थानीय डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने लापरवाही के आरोप में ड्रग कंट्रोलर और उनके तीन जूनियर को निलंबित किया है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जहां जनहित याचिका दायर कर सीबीआई जांच की मांग की गई है। सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। अब जानते हैं दवाओं का बाजार में आने का सिस्टम क्या है?
देश में दवाओं के नियम के लिए संस्था
भारत में दवाओं के रेगुलेशन से जुड़ी संस्थाएं दो स्तरों पर काम करती हैं — केंद्रीय और राज्य स्तर पर। भारत में दवाओं की बिक्री, बनाने और मार्केटिंग को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) अधिकृत सरकारी संस्था है। यह संस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करती है।
-
CDSCO नई दवाओं की मंजूरी देता है। इसके प्रमुख अधिकारी को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) कहा जाता है।
- दवा के निर्माण, आयात और बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की निगरानी करता है।
- स्टेट ड्रग कंट्रोलर के साथ मिलकर दवा की क्वालिटी और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- फार्माकोविजिलेंस और दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी करता है।
अन्य केंद्रीय संस्थाएं:
नेशनल फार्मासुटिकल प्राइसिंग ऑथिरिटी (NPPA) जो दवाओं के प्राइसिंग और निगरानी का कार्य करता है।
नेशनल मेडिकल काउंसिल डॉक्टरों के आचार संहिता को लागू करता है।
राज्य स्तर पर, स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट अपने-अपने राज्यों में दवाओं की खुदरा और थोक बिक्री के लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा दवा दुकानों की जांच, और गैरकानूनी दवाओं की रोकथाम इसका कार्य होता है।
यह भी पढ़ें- खुदकुशी से पहले IPS वाई पूरन के घर में क्या-क्या हुआ?
दवा को बाजार में लाने का प्रोसेस
भारत में किसी भी नई दवा को बाजार में लाने के लिए CDSCO एक केंद्रीय संगठन है। यह संस्था यह सुनिश्चित करती है दवा सुरक्षित, प्रभावी और हाई क्वालिटी वाली हो। इसमें दवा के अप्रुवल के लिए कागजी कार्रवाई के साथ-साथ कई तरह के लाइसेंस की जरूरत रहती है। यह सभी नियम 1940 के अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत आते हैं। किसी भी नई दवा की स्वीकृति कैसे मिलती है?
- यह प्रक्रिया CDSCO के प्रमुख DCGI से अनुमति मिलने के साथ शुरू होती है। आवेदन ऑनलाइन प्लैटफॉर्म SUGAM पोर्टल के जरिए की जाती है। दुनिया के मानक स्तर के हिसाब से दवा कंपनी को अपना विस्तृत डेटा देना होता है। फिर एक समिति इसका मूल्यांकन करती है।
- नई दवा को मंजूरी मिलने के बाद कंपनी को उसके प्रोडक्शन और बिक्री के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने होते हैं। भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों को CDSCO और संबंधित राज्य लाइसेंसिंग बॉडी से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है।
- यह लाइसेंस इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) और सभी मानकों का पालन कर रही है। वहीं, विदेशी कंपनी अपनी दवा भारत में बेचने के लिए किसी अधिकृत एजेंट के माध्यम से आयात लाइसेंस प्राप्त करते हैं।
- लाइसेंस मिलने के बाद दवा को बाजार में उतारने की अनुमति मिलती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया जारी रहती है। NPPA आवश्यक दवाओं की कीमतों की निगरानी करता है ताकि वे किफायती बनी रहें।
अब सवाल उठता है कि कोई भी डॉक्टर मरीजों किस आधार पर दवाओं को प्रिसक्राइब करते हैं? डॉक्टर आमतौर पर क्लिनिकल गाइडलाइन्स और मेडिकल रिसर्च डेटा के आधार पर दवा चुनते हैं। इसके अलावा, सरकार द्वारा जारी की गई नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन (NLEM) भी डॉक्टरों को दवा चुनने में मदद करती हैं। एमआर फार्मास्युटिकल कंपनियों के प्रतिनिधि होते हैं। उनका काम डॉक्टरों को नई दवाओं, उनके उपयोग, असर और दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी देना होता है। हालांकि, कई बार एमआर डॉक्टरों को अपनी कंपनी की दवा लिखने के लिए प्रमोशनल ऑफर और गिफ्ट जैसे लालच देते हैं, यही हिस्सा अक्सर विवादों में रहता है।