6 अप्रैल 2025। दिल्ली की किराड़ी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अनिल झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दिल्ली की डबल इंजन सरकार ने दिल्ली के बच्चों का हक मारकर करावल नगर के एक सरकारी स्कूल में 10 रोहिंग्या बच्चों को एडमिशन दे दिया है। एक तरफ भाजपा रोहिंग्या को लेकर हंगामा करती है तो दूसरी तरफ उनको समर्थन देती है। भाजपा को भारत के गरीबों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बजाय रोहिंग्याओं की चिंता है, इसलिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में रोहिंग्या बच्चों को एडमिशन दे दिया गया। आम आदमी पार्टी इसका विरोध और जांच की मांग करती है। कुछ ऐसे ही आरोप भाजपा, आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार पर लगाती थी।
दो पार्टियों की सियासी जंग के बीच सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या किसी बच्चे को शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित किया जा सकता है, वही भी इस आधार पर कि वह इस देश का नागरिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की एक NGO की याचिका पर एक अहम फैसला 12 फरवरी 2025 को सुनाया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'शिक्षा का अधिकार सार्वभौमिक है और किसी भी बच्चे के साथ शिक्षा में भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिसमें दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थी बच्चे भी शामिल हैं।'
सु्प्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2025 को निर्देश दिया, 'रोहिंग्या बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन करें। अगर स्कूल दाखिला देने से इनकार करते हैं, तो वे दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि दाखिले के लिए पहले पात्रता की जांच होनी चाहिए।'

यह भी पढ़ें: रोहिंग्या बच्चों को कैसे मिला पढ़ाई का हक? कानून समझिए
देश को कैसे मिला शिक्षा का अधिकार?
सुप्रीम कोर्ट ने जिस 'शिक्षा के अधिकार' का हवाला दिया था, उसके बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। पहले शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकारों में शामिल नहीं था, यह राज्य के नीति निदेशक तत्वों की सूची में आता था। संविधान में मूल रूप से शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं किया गया था।
संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व, बाध्यकारी नहीं हैं, इन्हें कानूनी रूप से अदालतों के जरिए स्थापित नहीं कराया जा सकता। लंबी बहस और कानूनी लड़ाई के बाद शिक्षा का अधिकार, बुनियादी अधिकारों में शामिल हुआ। 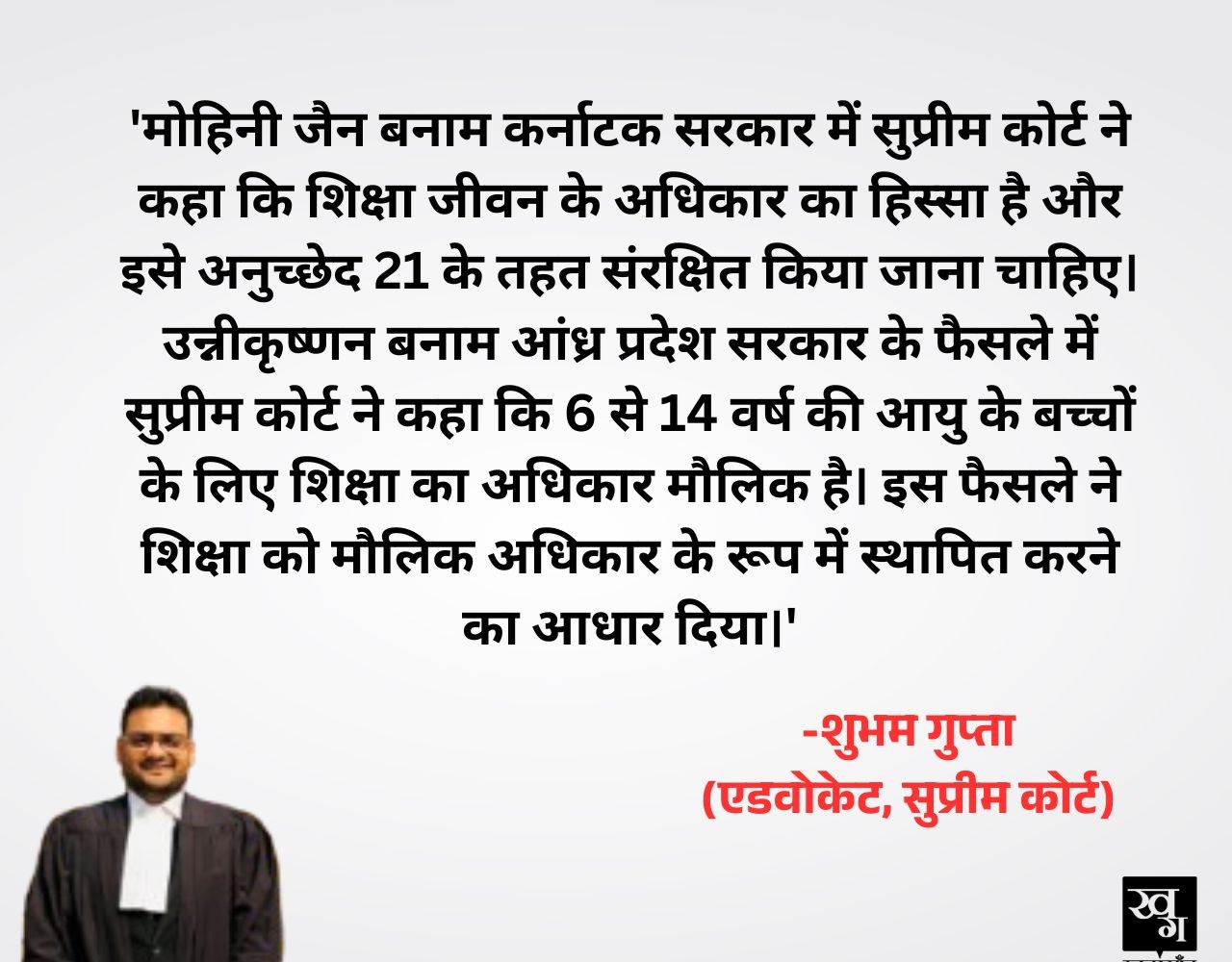
आखिर अनुच्छेद 21ए और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के आने की कहानी क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं।
कैसे मूल अधिकारों में शामिल हुई शिक्षा?
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शुभम गुप्ता खबरगांव के साथ बातचीत में कहा, 'देश में ज्यूडिशियल एक्टिविज्म के चलते कई कानून अस्तित्व में आए। उनमें सबसे अहम अधिकार अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा का अधिकार था। यह संसद से बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन बहुत देरी से आया। अनुच्छेद 21ए के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। RtE एक्ट मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बारीकियों पर विस्तार से प्रकाश डालता है, जिसमें सरकार की जिम्मेदारियां, प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और स्कूलों के लिए मानक, और शिक्षा के अधिकार की निगरानी और प्रवर्तन के लिए तंत्र शामिल हैं।'
यह भी पढ़ें: दिल्ली: निजी स्कूलों में फीस कम कराना मुश्किल? कानूनी दांव-पेच समझिए
कैसे पड़ी शिक्षा के अधिकार की नींव?
शिक्षा के अधिकार की नींव में दो मामलों ने अहम भूमिका निभाई। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार 1992 और उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार 1993।
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता शुभम गुप्ता ने कहा, 'मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा जीवन के अधिकार का हिस्सा है और इसे अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक है। इस फैसले ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करने का आधार दिया।'

क्यों कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत इसकी व्याख्या की?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वंतत्रता के अधिकार से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद में 21 कहता है, 'किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।'
अनुच्छेद 21ए कहता है, 'राज्य छह से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करेगा, उपबंध करेगा।'
मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक सरकार ने कहा था, 'शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत अंतर्निहित है। शिक्षा के बिना मानवीय गरिमा और जीवन की गुणवत्ता संभव नहीं है।'
उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार को परिभाषित किया। एडवोकेट शुभम गुप्ता ने कहा, '14 साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार माना, पर उच्च शिक्षा को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा के व्यावसायीकरण की निंदा की और राज्य को फीस और एंट्रेस एग्जाम के रेगुलेशन का अधिकार दिया।'
एडवोकेट शुभम गुप्ता ने कहा, 'प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के लिए सीट रिजर्व करने का प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत किया गया है। इस अधिनियम की धारा 12(1)(C) कहती है कि प्राइवेट स्कूल अपनी कुल सीटों का कम से कम 25% हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रखें और मुफ्त शिक्षा दें। यह नियम नर्सरी और कक्षा 1 जैसी प्रवेश-स्तरीय कक्षाओं पर लागू होता है। यह कितना सफल हुआ, इस पर लंबी बहस हो सकती है।'
संसद से कैसे बना कानून?
एडवोकेट शुभम गुप्ता ने कहा, 'साल 1950 तक, शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं किया गया था। अनुच्छेद 45 में केवल यह प्रावधान था कि राज्य 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। साल 1990 के दशक में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की मांग उठने लगी।'
दीवान लॉ कॉलेज में विधि विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर निखिल गुप्ता ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट पहले ही मोहिनी जैन केस में कहा था कि शिक्षा अनुच्छेद 21 का हिस्सा है और इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इन इस फैसले ने सरकार पर शिक्षा को कानूनी रूप से लागू करने का दबाव बनाया।'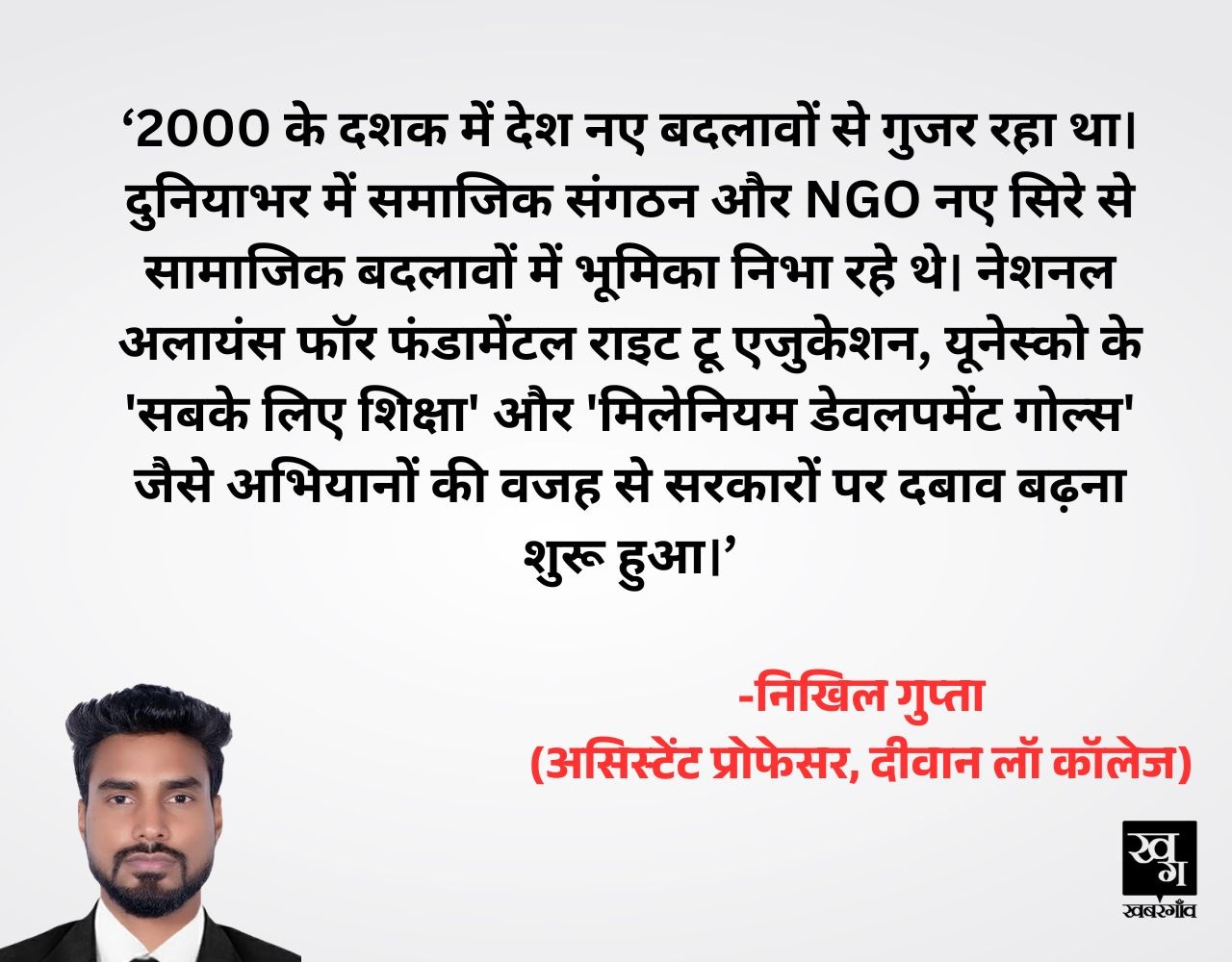
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्याल में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विकास कुमार ने कहा, 'संसद में साल 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। संसद ने दिसंबर 2002 में 86वां संविधान संशोधन पारित किया। नए संशोधन के बाद अनुच्छेद 21ए जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। संसद से अनुच्छेद 45 को संशोधित कर 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल पर जोर दिया गया। संविधान में अनुच्छेद 51A(k) जोड़ा गया, जिसमें माता-पिता की जिम्मेदारी तय की गई कि वे अपने बच्चों की शिक्षा तय करें।'
कैसे बना राइट टू एजुकेशन एक्ट?
असिस्टेंट प्रोफेसर निखिल गुप्ता ने कहा कि अनुच्छेद 21A को लागू करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचे की जरूरत थी। केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ नए सिरे से बातचीत शुरू की। लंबी बैठकें चलीं, साल 2005 में, केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड (CABE) ने एक समिति बनाई, जिसने RTE कानून का शुरुआती मसौदा तैयार किया।
असिस्टेंट प्रोफेसर विकास कुमार ने कहा, 'मसौदे में कई संशोधन और लंबी बहस के बाद मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को संसद में अगस्त 2009 में पारित किया गया। यह कानून 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ।'

और किन संगठनों ने उठाई थी मांग?
संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ असिस्टेंट प्रोफेसर निखिल गुप्ता ने कहा, '2000 के दशक में देश नए बदलावों से गुजर रहा था। दुनियाभर में समाजिक संगठन और NGO नए सिरे से सामाजिक बदलावों में भूमिका निभा रहे थे। नेशनल अलायंस फॉर फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, यूनेस्को के 'सबके लिए शिक्षा' और 'मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स' जैसे अभियानों की वजह से सरकारों पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ।'
देश में सर्व शिक्षा अभियान (2000) जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों की शुरुआत हुई तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की मांग ने जोर पकड़ा। यह वे अहम बदलाव थे जिन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम की नींव को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई और 1 अप्रैल 2010 तक देश के बच्चों को यह अधिकार मिला।
राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या है?
सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता शुभम गुप्ता ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट की सबसे अहम बात यह है कि यह 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवर्य शिक्षा के अधिकार की वकालत करता है। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि हर 6-14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिलेगा। धारा 6 कहती है कि राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल बनाएं। धारा 7 केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय जिम्मेदारी से संबंधित है।
राइट टू एजुकेशन एक्ट की धारा 8 और 9 कहती है कि सरकारें यह तय करें कि कोई बच्चा आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न हो। धारा 14 कहती है कि अगर किसी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र न हो तो उसे एडमिशन देने से इनकार न किया जाए। रोहिंग्या बच्चों के एडमिशन से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पीछे धारा 14 को भी अहम माना जाता है। 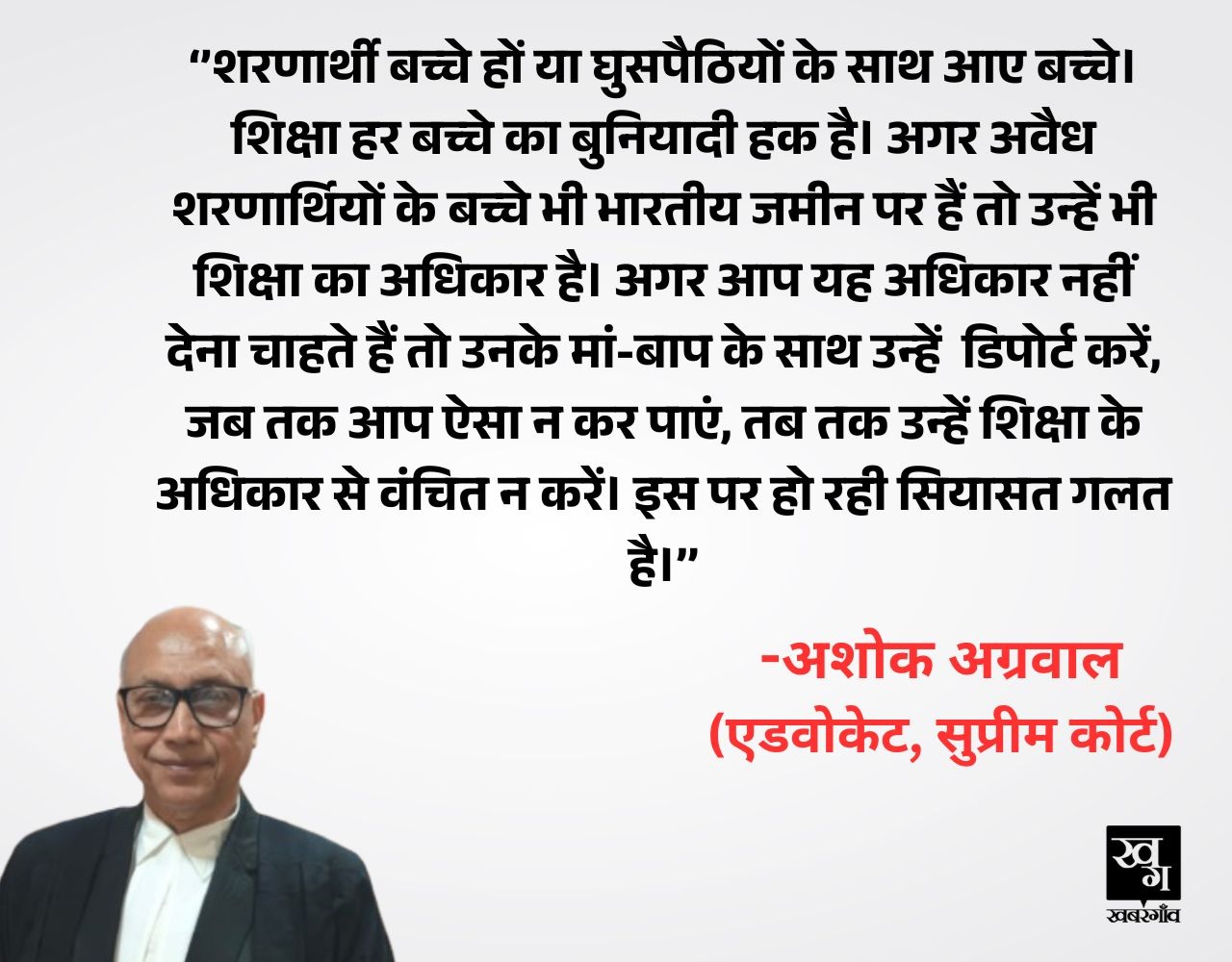
चर्चा में क्यों है शिक्षा का अधिकार?
दिल्ली में रोहिंग्या बच्चों के स्कूल में एडमिशन को लेकर सियासी बवाल मचा है। आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने हाल ही में कहा था कि दिल्ली में रोहिंग्या छात्रों को एडमिशन दिया गया है। भारत के बच्चों का हक मारकर रोहिंग्या छात्रों को एडमिशन दिया गया है। यह किस नियम के तहत किया गया है। रोहिंग्या छात्रों को एडमिशन क्यों दिया गया है?
दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनावी जनसभाओं में जमकर कहते थे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अवैध प्रवासियों को बढ़ावा दिया है और उनके दस्तावेज बनवाए हैं जिससे वे अपने वोट बैंक को बढ़ा सकें।
दोनों पार्टियों की सियासी बहस में अहम बात यह है कि शिक्षा के अधिकार से चाहे नागरिक हों या शरणार्थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। जब तक वे भारत की धरती पर हैं, यह उनका बुनियादी हक है, जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है।

भारत में कितने रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं?
UNHRC के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 22 हजार 500 रोहिंग्या शरणार्थी उसके पास रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 676 रोहिंग्या शरणार्थी भारत के अलग-अलग हिस्सों में हिरासत केंद्रों में बंद हैं। दिल्ली में 10 रोहिंग्या बच्चों को हाल ही में एक स्कूल में एडमिशन मिला है, जिसके बाद अब इस पर सियासत हो रही है।
