मगध और वैशाली जैसे महाजनपदों से बिहार राज्य कैसे बना? पढ़िए इतिहास
बिहार का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है। कभी यहां महाजनपद रहे तो कभी मुगलों ने राज किया, कभी अंग्रेजों का शासन आया तो आजादी की जंग का प्रमुख केंद्र भी बिहार ही रहा।
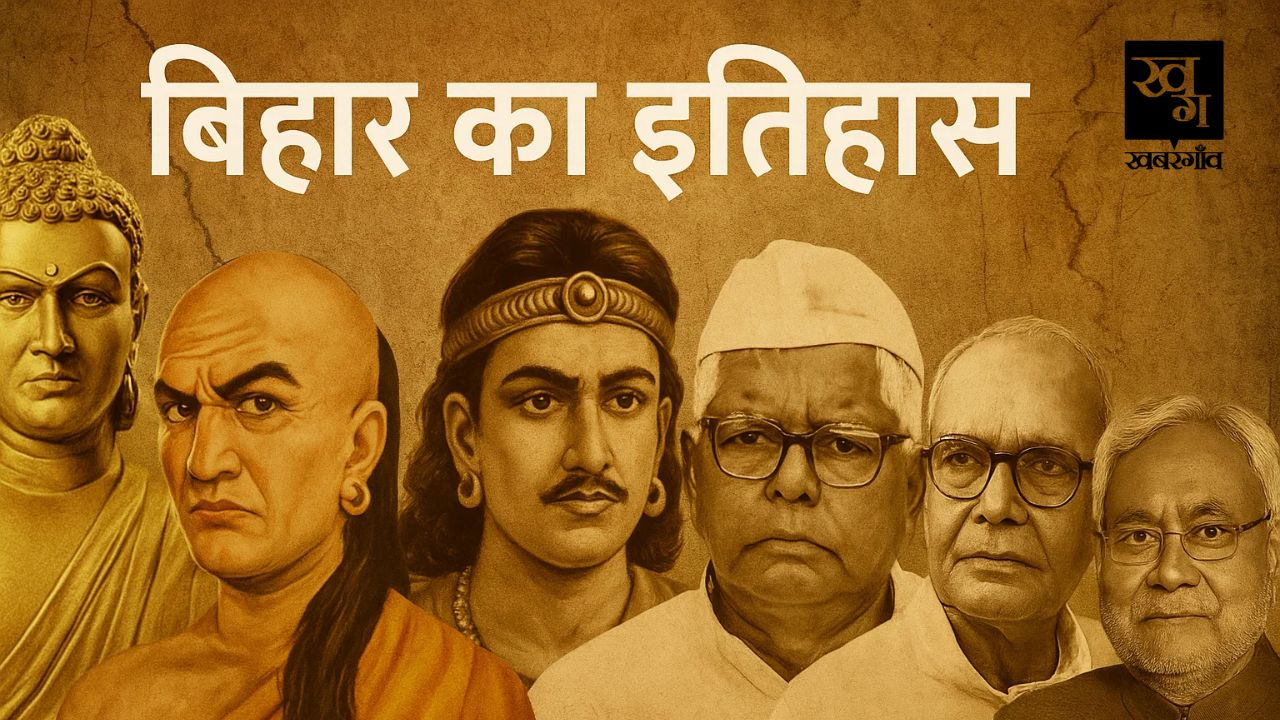
बिहार का इतिहास, Photo Credit: Sora AI
बिहार, सम्राट अशोक के पराक्रम की ज़मीन। बुजुर्गों की जुबान में बुद्ध की धरती। इतिहास की भाषा में गांधीगीरी के प्रथम प्रयोग की माटी। हिंदुस्तान का वह हिस्सा जहां नालंदा विश्वविद्यालय की ओट लिए दुनियाभर के बच्चे पढ़ाई करते थे। आर्य भट्ट का घर जिसने दुनिया को बताया कि शून्य जैसी एक चिड़िया भी होती है। एक ऐसा सूबा जिसकी छाती अपने इतिहास और परंपरा से फूले नहीं समाती है लेकिन इतराने के ठीक उसी पहर में कहानियां हमसे दो पीढ़ी पहले की भी सुनने को मिलने लगती हैं। बुद्ध की ज़मीन से खूनी अतीत की चीत्कार सुनाई पड़ती है। श्रुति परंपरा से लेकर लिखित इतिहास तक बिहार के हिस्से का कोना-कोना शांति के उपदेश के साथ साथ दहशत से भी भरा हुआ है। अजीब विंडबना का समन्वय है। ये सारी घटनाएं जिस छतरी के नीचे खुद को समेटे हुए हैं उन्हें पुरनियों ने कहानी की संज्ञा दी।
इन सिलसिलों का पहला पन्ना खुलता है 305 ईसा पूर्व। सिकंदर के बाद ताकत आई सेल्युकस के हाथ। उसने पंजाब और सिंध के इलाकों पर कब्जा जमाया। धीरे-धीरे भारत के उत्तर पश्चिमी भाग के ज़्यादातर इलाके पर सेल्युकस का राज हो गया। तब पाटलिपुत्र यानी कि आज के पटना में एक सम्राट का शासन था। जिसने हज़ारों किलोमीटर का सफर तय करके सेल्युकस के खिलाफ युद्ध लड़ा। सेल्युकस को इस युद्ध में भारी नुकसान हुआ। जंग हारकर सेल्युकस ने शांति का प्रस्ताव रखा। इसके तहत सेल्युकस ने राजा को उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पश्चिमी हिस्सा दे दिया। राजनीति और कूटनीति पल-पल बदलती है। इसीलिए शांति को स्थायी रखने के लिए इसे एक रिश्ते में बांधा गया। सेल्युकस ने अपनी बेटी की शादी पाटलिपुत्र से आए उस सम्राट से करा दी। सम्राट का नाम - चंद्रगुप्त मौर्य। जो कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक 'मगध' के सम्राट थे। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र।
यह भी पढ़ें- UN, गुजरात फिर बिहार, आखिर प्रशांत किशोर की पूरी कहानी क्या है?
मगध साम्राज्य सीरीज की इस पहली किस्त में कहानी मगध साम्राज्य के इतिहास की। कैसे पाटलिपुत्र और राजगीर से मगध के सम्राटों ने सिर्फ आज के भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल, बलूचिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान, तक शासन किया। मगध साम्राज्य सीरीज में हम बिहार के अतीत से लेकर वर्तमान तक यात्रा करेंगे। उसके समाज और उसकी राजनीति को समझेंगे। हम राजाओं के योद्धाओं के किस्से आपको बताएंगे। उनके बाद मुगल और फिर कंपनी बहादुर के राज पर नज़र डालेंगे और फिर आज़ाद भारत में बिहार की राजनीति पर तो बहुत विस्तार से बात होनी है।
महाजनपद और बिहार
करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान
रसरी आवत जात ते, सिल पर पड़त निसान
यह दोहा ब्रज भाषा का है और लिखा कवि वृंद ने लेकिन यह सबसे ज़्यादा जोड़कर सुनाया जाता है पाणिनी की कहानी से। लोककथाएं कहती हैं कि बचपन में पढ़ने में कमज़ोर पाणिनी ने कुएं पर रस्सियों के निशान देखे, तब समझ आया कि मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसके बाद पाणिनी ने मेहनत की और कालांतर में वह भाषाविद हुए। अष्टाध्यायी रची, जिसके 3 हज़ार 996 छंदों में आपको संस्कृत व्याकरण के सूत्र मिलते हैं लेकिन पाणिनी सिर्फ व्याकरण के ही ज्ञाता नहीं थे। लॉजिक और फिलॉसफी में भी उनकी बड़ी दिलचस्पी थी और जो कुछ उन्होंने लिखा, उसमें अपने समय को दर्ज भी करते गए।
पाणिनी की इसी स्कॉलरशिप में आपको 40 या कभी-कभी उससे भी ज़्यादा जनपदों का ज़िक्र मिलता है। पाणिनी कब हुए थे, उसे लेकर इतिहासकार एकमत नहीं हैं लेकिन यह बात ईसा से 500 से 400 साल पुरानी तो ज़रूर है। जनपदों का इतिहास तो इससे भी एक हज़ार साल पुराना है। इन जनपदों को आप छोटे-छोटे सूबों की तरह समझ सकते हैं, जिनमें हर स्तर पर प्रशासन विकसित हो चुका था। ये कबीले नहीं थे। राजा था तो राजा को सलाह देने के लिए सभा होती थी। आज शहरों में जिस तरह म्युनिसिपैलिटी होती है, वैसी व्यवस्था जनपदों में भी थीं और गांव के स्तर पर भी प्रशासन के कुछ ढांचे थे। हर जनपद अपने आप में नायाब। कहीं मोनार्की माने राजशाही थी, कहीं आज के ब्रिटेन की तरह कॉन्स्टीट्यूश्नल मोनार्की थी तो कोई जनपद गणतंत्र भी थे, माने रिपब्लिक।
यह भी पढ़ें- सदियों का इतिहास, सैकड़ों ऐतिहासिक स्थल, टूरिज्म में पीछे क्यों बिहार?
ये जनपद आज के हिंदुस्तान-पाकिस्तान के साथ-साथ अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग तक फैले हुए थे। राजनीति और कूटनीति तब भी उतने ही भारी कीवर्ड थे तो युद्ध होते रहते थे और इनके साथ जनपदों की संख्या बदलती रहती थी। वक्त के साथ ताकतवर जनपदों ने दूसरी जनपदों को अपने में मिलाया और इस तरह बुद्ध के समय तक 16 महाजनपद अस्तित्व में आए- काशी, कोसल, अंग, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कुरू, पंचला, मत्स्य, सुरासेन, असाका, अवंति, गंधारा, कंबोज और मगध।
मगध का इतिहास
इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था मगध। आज बिहार में जिसे मगध प्रमंडल कहते हैं, उसमें पांच ही ज़िले आते हैं- जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और अरवल लेकिन भाषा और संस्कृति के हिसाब से देखेंगे तो जैसे पटना और नालंदा के इलाके भी इसमें जुड़ जाते हैं। पाटलिपुत्र में तो जहां मगध की राजधानी ही थी। इसके अलावा शेखपुरा और लखीसराय दो जिले हैं, जिसे सांस्कृतिक रूप से मगध का हिस्सा माना जाता है। खैर अतीत में लौटते हैं।
आज जिसे हम बिहार कहते हैं, उस भौगोलिक विस्तार में मगध के अलावा अंग, वज्जि और लिच्छवी तीन मजबूत साम्राज्य थे। मगध ने अपने पड़ोसी अंग को बहुत जल्दी ही जीतकर अपने में ले लिया था। गंगा के पूर्वी भाग में वज्जि था। वज्जि या वृज्जि एक संघ था, माने कनफेडरेसी। यह कई कुलों से मिलकर बना था - लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक वगैरह। यह कुछ-कुछ वैसा ही था, जैसे आज का संयुक्त अरब अमीरात या UAE है। वृज्जि एक गणराज्य था, जिसका मतलब हुआ कि इसका शासन राजा द्वारा नहीं, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। उनकी शासन प्रणाली को 'गण' या 'संघ' कहा जाता था। ईसा से 600 साल पहले वृज्जि अस्तित्व में था। इसीलिए इस गणतंत्र को दुनिया में लोकतंत्र की ओर बढ़ पहले कदमों की तरह देखा जाता है। कुछ कुछ ग्रीस की तरह। जहां राजा नहीं, जनता ताकतवर होती है।
यह भी पढ़ें: न बड़े उद्योग, न तगड़ा रेवेन्यू, कैसे चलती है बिहार की अर्थव्यवस्था?
वृज्जि में सबसे ताकतवर कुल था लिच्छिवी, जिनका गढ़ वैशाली, वृज्जि संघ की राजधानी थी। यह नाम आपने खूब सुना भी होगा। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली के रेफरेंस में। वैशाली के बगल में मगध था, जो उसे खुद में मिलाना चाहता था। अजातशत्रु ने खूब प्रयास किए। कहानी कहती है कि एक हमले के दौरान अजातशत्रु घायल हो गया। तब उसे आम्रपाली ने पनाह दी। वह जानती नहीं थी कि वह दुश्मन के घाव भर रही है। दोनों जवान थे तो प्यार हो गया। जब आम्रपाली को मालूम चलता है कि उसने अपना दिल दुश्मन को दे दिया, तो वह अजातशत्रु से मांगती है कि मगध की सेनाएं लौट जाएं और वैशाली को बख्श दिया जाए।
अजातशत्रु लौटा लेकिन वैशाली के लोग उसके और आम्रपाली के बारे में जान गए तो उन्होंने अपनी नगरवधु को कैद कर लिया। अजातशत्रु का दिल भी टूटा और उसे वैशाली पर चढ़ाई का बहाना भी मिल गया। आम्रपाली को आज़ाद करने के लिए उसने सब बर्बाद कर दिया। जब अंततः आम्रपाली आज़ाद हुई तो चारों तरफ तबाही और खून देखकर टूट गई और उसने बुद्ध का रास्ता चुन लिया। अनुयायी बन गई। संभवतः इसी कहानी के चलते महाजनपदों का ज़िक्र आते ही लोग वैशाली का नाम ले लेते हैं, भले ही वह वृज्जि के भीतर एक ताकतवर कुल था। मगध और वृज्जि से इतर आसपास के दो बड़े साम्राज्य काशी और कोसल थे। वत्स भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कौशांबी थी। इन सारे महाजनपदों का विस्तार आधुनिक भारत के अलग-अलग राज्यों तक था।
मगध साम्राज्य की स्थापना
अब आते हैं मगध पर। इसकी स्थापना का श्रेय जाता है, हर्यंक वंश के राजा बिंबिसार को। बिंबिसार का दौर 558 से 491 ईसा पूर्व तक था। बिंबिसार ने मगध के विस्तार के लिए कई योजनाओं पर काम किया। मगध के विस्तार के लिए उन्होंने अलग-अलग साम्राज्य के साथ वैवाहिक गठबंधन किया। बिंबिसार की तीन पत्नियां थीं। खेमा, चेलाना और वैदेही। खेमा को कोसलदेवी के नाम से भी जाना जाता था। वह कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन थीं। बिंबिसार ने इस शादी से मगध और कोसल के बीच एक मजबूत गठबंधन बना लिया था। बिंबिसार की दूसरी पत्नी का नाम था चेलाना, जो लिच्छवी की राजकुमारी थीं और अजातशत्रु की मां भी। इतिहासकार रामशरण शर्मा अपनी किताब, 'भारत के प्राचीन इतिहास' में लिखते हैं कि बिंबिसार की तीसरी पत्नी का नाम था वैदेही, जो मगध के तहत आने वाले विदेह की राजकुमारी थीं।
बिंबसार ने एक शादी पंजाब के मद्रा वंश की राजकुमारी नंदनी से भी की थी। मद्रा वंश का साम्राज्य रावी और चेनाब नदी के बीच में पड़ता था और इसकी राजधानी थी, सागल यानी कि आज का सियालकोट। इसका विस्तार आज के भारत के पंजाब और हरियाणा तक था। इन साम्राज्यों की राजकुमारियों से शादी करके बिंबिसार ने अपार कूटनीतिक प्रतिष्ठा हासिल की और मगध के पश्चिम और उत्तर की ओर विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया।
यह भी पढ़ें- हजारों करोड़ की घोषणाएं कर चुके नीतीश, बिहार झेल पाएगा आर्थिक बोझ?
आम्रपाली की कहानी ने वैशाली से हुई लड़ाई को मशहूर कर दिया लेकिन सच यह है कि मगध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, अवंती। अवंती और मगध लगभग बराबर ताकतवर थे। बिंबिसार के समय मगध और अवंती के बीच एक युद्ध हुआ। मगर युद्ध शुरू होने से कुछ ही दिनों बाद शांति समझौता हो गया। समझौता ऐसा कि जब युद्ध के बाद वहां के राजा चंद प्रद्योत महासेन को जॉन्डिस हुआ, तो उन्होंने बिंबिसार से एक अच्छे वैद्द की डिमांड की। तब बिंबिसार ने एक मशहूर वैद्य जिवाका को अवंती की राजधानी उज्जैन भेजा था। बिंबिसार भले ही अवंती को ना जीत पाए हों लेकिन अलग महाजनपदों के कई हिस्सों को अपने में मिला लिया था। बिंबिसार के शासनकाल यानी कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के पास लगभग 80 हजार गांव थे और वह तमाम 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था।
बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयिन
बिंबिसार के शासन में मगध की राजधानी थी गिरिवराज, जिसे आज राजगीर या राजगृह के नाम से जाना जाता है। राजगीर चारों तरफ से पहाड़ों से गिरा था और अंदर घुसने के सभी रास्ते पत्थर की दीवार से बंद थे, जिसने राजधानी को अभेद्य बना दिया था लेकिन बिंबसार सिर्फ लड़ाई ही नहीं जानते थे। उन्होंने बुद्ध और महावीर की शिक्षाओं का भी प्रसार किया। बौद्ध और जैन धर्म के लिए मठों का भी निर्माण कराया। बौद्ध इतिहास के मुताबिक बिंबिसार ने मगध पर 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था।
इसके बाद मगध के अगले सम्राट हुए अजातशत्रु। गद्दी पर बैठने के लिए उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार ने अपने शासन में कूटनीति को ज्यादा तरजीह दी थी लेकिन अजातशत्रु ने मगध के विस्तार के लिए ताकत का इस्तेमाल ज्यादा किया। काशी और कोसल का साम्राज्य अजातशत्रु की इस नीति के खिलाफ हो गया और दोनों ने मिलकर अजातशत्रु के खिलाफ युद्ध लड़ा। हालांकि, अजातशत्रु भारी पड़े। एक तरफ जहां बिंबिसार ने कोसल की राजकुमारी से शादी करके कूटनीतिक रूप से कोसल के साथ गठबंधन किया था, वहीं अजातशत्रु अपनी ताकत से उसे मगध में जोड़ना चाहते थे। खैर इस युद्ध में अजातशत्रु की जीत हुई। कोसल के राजा को शांति प्रस्ताव के लिए अपनी एक बेटी की शादी अजातशत्रु से करानी पड़ी और काशी पर से अपना पूर्ण अधिकार भी छोड़ना पड़ा था।
गद्दी के लिए अपने पिता को मारने वाले अजातशत्रु के लिए रिश्तों के कोई मायने नहीं थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि अजातशत्रु की मां चिलाना लिच्छवी साम्राज्य की राजकुमारी थीं लेकिन अजातशत्रु ने लिच्छवी के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया क्योंकि लिच्छवी और कोसल के राजाओं के अच्छे संबंध थे और कूटनीतिक स्तर पर भी दोनों एक-दूसरे के साथी थे। मगर अजातशत्रु के खून में बस मगध का विस्तार था। जिसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते थे। अजातशत्रु ने लिच्छवी को भी युद्ध में हराया और मगध साम्राज्य का विस्तार काशी और वैशाली तक कर लिया। दंतकथाएं कहती हैं कि अजातशत्रु के रथ में एक गदा जुड़ा हुआ था। रथ दुश्मन सैनिकों के बीच से निकलता था तो गदा की चपेट में कई दुश्मन सैनिक आ जाते।
अजातशत्रु के लिए सबसे बड़ी चुनौती था अवंती साम्राज्य। मगर बिंबिसार को जब लगा कि दोनों के लिए एक दूसरे को जीतना आसान नहीं है, तो उन्होंने शांति समझौता कर लिया लेकिन अजातशत्रु के आक्रामक रवैये से उसके कूटनीतिक रिश्ते सबसे खराब होते चले गए थे। अजातशत्रु के समय में ही अवंती ने वत्स को हराकर कौशांबी पर कब्जा कर लिया था। अब नज़र थी मगध पर। अवंती के राजा ने अजातशत्रु को अपना विस्तार मगध तक करने की धमकी दी। इस खतरे के डर से अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी शुरू कर दी थी। इन दीवारों के अवशेष राजगीर में आज भी देखे जा सकते हैं। हालांकि, उनके जीते जी अवंती ने कभी आक्रमण नहीं किया।
अजातशत्रु के बाद मगध की कमान संभाली उदयिन या उदयभद्र ने। बिल्कुल उसी तर्ज पर जैसे अजातशत्रु ने संभाली थी। उदयिन हर्यंक वंश के तीसरे राजा और अजातशत्रु के बेटे थे। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी संभाली थी। ठीक उसी तरह उदयिन ने भी अजातशत्रु की हत्या कर सत्ता संभाली।
सम्राट बनने के बाद उदयिन ने सबसे पहला काम किया - राजधानी को शिफ्ट करना। राजगीर पर हमले का खतरा था तो उदयिन राजधानी को गंगा और सोन नदियों के संगम पर ले आए- पाटलिपुत्र या आज का पटना। उदयिन के इस कदम ने एक ऐसे शहर की नींव रखी जो मौर्य साम्राज्य के दौरान सदियों तक एक प्रमुख राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बना रहा। इसकी भौगोलिक स्थिति ने व्यापार, रक्षा और केंद्रीकृत नियंत्रण को बढ़ाया, जिससे मगध का प्रभुत्व मजबूत हुआ।
जैन धर्म के अनुयायी के रूप में उदयिन ने हर्यंक वंश की जैन धर्म के प्रति समर्थन की परंपरा को जारी रखा, जिससे मगध में बौद्ध धर्म के साथ-साथ जैन धर्म का भी सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव बढ़ता रहा। अपने पिता की तरह उदयिन ने भी अवंती के साथ लड़ाई की और इसके राजा पालक को कई बार पराजित किया। हालांकि, बौद्ध स्रोतों के अनुसार 444 ईसा पूर्व में उदयिन के बेटों ने उनकी हत्या कर दी। वैसे जैन स्रोत मानते हैं कि उदयिन की मौत के पीछे अवंती का हाथ था।
उदयिन अपने पिता अजातशत्रु या दादा बिंबिसार जितने प्रभावी नहीं थे। इसलिए यहीं से हर्यंक वंश का ढलान शुरू हो गया। इसके बाद शिशुनाग वंश ने मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। मगर इसको लेकर अलग-अलग दावे हैं। जैन परंपरा में कहा गया है कि उनकी हत्या दुश्मन साम्राज्य के राजा ने की थी। बौद्ध ग्रंथों में ज़िक्र है कि हर्यंक वंश में अजातशत्रु से लेकर नगाडसाका सबने अपने पिता की हत्या करके मगध पर शासन किया था।
खैर सबसे बड़ी मान्यता यही है कि उदयिन के बाद शिशुनाग वंश ने मगध की कमान संभाली थी। शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता थी अवंती पर जीत। लगभग सौ सालों बाद मगध और अवंती की राइवलरी अवंती की हार के साथ खत्म हुई। शिशुनाग के शासनकाल में अवंती मगध का हिस्सा बना और मौर्य काल तक मगध के साथ ही रहा।
सिकंदर की सेना का आगे बढ़ने से इनकार
शिशुनाग के बाद मगध पर नंद वंश का शासन रहा। नंद वंश के दौरान मगध और शक्तिशाली साम्राज्य बना। महापद्म नंद, नंद वंश के पहले शासक थे। इतने शक्तिशाली कि पंजाब और सिंध पर कब्जा करने वाला सिकंदर भी डर से मगध की तरफ कभी नहीं बढ़ा। महापद्म नंद, जिन्हें उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। पुराणों के अनुसार, उन्होंने कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जिनमें कलिंग (वर्तमान ओडिशा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा) भी शामिल है। उनकी उपलब्धियों में से एक प्रमुख उपलब्धि थी कलिंग के राजा को हराना और इस क्षेत्र को मगध साम्राज्य में शामिल करना। महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। हथिगुम्फा शिलालेख और पुराणों जैसे स्रोतों के अनुसार, उन्होंने कलिंग में एक नहर का निर्माण किया और वहां से एक जैन मूर्ति को विजय के प्रतीक के रूप में मगध ले गए। यह विजय उनकी सैन्य शक्ति और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। कहा जाता है कि उन्होंने ना सिर्फ कलिंग बल्कि कोसल को भी मगध में शामिल कर लिया था।
महापद्म नंद की सेना में लगभग 2 लाख पैदल सैनिक, 60,000 घुड़सवार सेना और 6000 लड़ाकू हाथी थे, जो उनकी सैन्य ताकत को किसी भी और साम्राज्य से मजबूत बनाता था। इस विशाल सेना ने उन्हें कई क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने में मदद की।
इतनी विशाल सेना का डर ही था जो अलेक्जेंडर ने मगध की तरफ बढ़ने की इच्छा त्याग दी। हालांकि, इसकी एक बड़ी वजह बताई जाती है कि अलेक्जेंडर की सेना को उत्तर भारत का एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पसंद नहीं आ रहा था और वे लगातार लड़ते-लड़ते बहुत थक गए थे इसलिए अलेक्जेंडर अपनी सेना लेकर वापस लौट गए। धीरे-धीरे नंद वंश के उत्तराधिकारियों की नेतृत्व क्षमता भी कमजोर पड़ती गई। घनानंद इस वंश के आखिरी शासक हुए। इसके बाद मौर्य वंश का शासन आया है, जिसमें मगध की ग्लोरी एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई।
मौर्य वंश का साम्राज्य
मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह एक बेहद ही साधारण परिवार से थे। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, उनका जन्म नंद राजवंश के दरबार में हुआ था। उनकी मां का नाम मूरा था जो एक शूद्र महिला थीं। हालांकि, एक पुरानी बौद्ध परंपरा के अनुसार, मौर्य गोरखपुर क्षेत्र में नेपाल तराई के पास पिप्फलिवना की एक छोटी गणतांत्रिक व्यवस्था के शासक वंश से थे। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के अंतिम दिनों में उनकी कमजोरियों का लाभ उठाया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सहायता से उन्होंने नंदों को उखाड़ फेंका और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के खिलाफ चाणक्य की चालों का विस्तृत वर्णन नौवीं शताब्दी में विशाखदत्त द्वारा लिखित नाटक मुद्राराक्षस में मिलता है।
इतिहासकार रामशरण शर्मा अपनी किताब में एक ग्रीक राइटर जस्टिन के हवाले से लिखते हैं कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों के साथ पूरे भारत पर राज किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन में कई छोटे-बड़े युद्ध जीते। जिनमें सबसे बड़ा था सेल्युकस के साथ लड़ा गया युद्ध। सेल्युकस अलेक्जेंडर की सेना में कमांडर थे। जो कि बाद में अलेक्जेंडर की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी बने। सेल्युकस के पास भारत के पूरे उत्तरी-पश्चिमी भाग पर कब्जा था। चंद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में मगध का विस्तार पूरे भारत तक करने का सोचा। चंद्रगुप्त और सेल्युकस के बीच युद्ध हुआ। मगर मगध की विशाल सेना के सामने सेल्युकस कहीं नहीं टिक पाया। सेल्युकस ने इस युद्ध में अपनी हार मानते हुए चंद्रगुप्त के सामने शांति का प्रस्ताव रखा। इस शांति प्रस्ताव में सेल्युकस ने अपनी एक बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कराई और उन्हें उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध का पूरा पश्चिमी भाग दे दिया। इस प्रस्ताव के तहत चंद्रगुप्त ने भी सेल्युकस को 500 हाथी दिए।
चंद्रगुप्त ने इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, जिसमें न केवल बिहार और उड़ीसा तथा बंगाल के बड़े हिस्से शामिल थे, बल्कि पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी भारत तथा दक्कन भी शामिल था। केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर, मौर्यों ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। मौर्यों ने अपने काल में उन गणराज्यों या संघों को भी जीता, जिन्हें कौटिल्य ने साम्राज्य के विकास में बाधा माना था।
चंद्रगुप्त के शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी विशाल सेना का रखरखाव। एक रोमन लेखक प्लिनी के अनुसार, चंद्रगुप्त ने 600,000 पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, और 9,000 युद्ध हाथी रखे हुए थे। एक अन्य स्रोत के अनुसार, मौर्यों के पास 8,000 रथ भी थे। ऐसा कहा जाता है कि मौर्य काल में मगध के पास अपनी नौसेना भी थी। मौर्यों की सैन्य शक्ति नंदों की तुलना में लगभग तीन गुनी थी।
मगर सबसे बड़ा सवाल कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी विशाल सेना के खर्चों को पूरा कैसे किया? यदि हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर भरोसा करें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य ने साम्राज्य की लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखा था। राज्य ने किसानों और शूद्र श्रमिकों की मदद से बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया। नई कृषि योग्य भूमि से पर खेती करने वाले किसानों से राज्य को अच्छा राजस्व प्राप्त होता था। मौर्य काल में किसानों से टैक्स के रूप में कुल उपज की एक चौथाई से लेकर छठे भाग तक अनाज लिया जाता था। जिन्हें राज्य द्वारा सिंचाई सुविधाएँ प्रदान की गई थीं, उन्हें इसके लिए अलग से भुगतान करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त आपातकाल के समय में किसानों को अधिक फसलें उगाने के लिए बाध्य किया जाता था।
लेकिन क्या टैक्स ही एकमात्र कारण था मगध के डॉमिनेंस का? नहीं। मगध के क्षेत्र में लोहे की कई खदाने थीं। जिसकी वजह से हथियार बनाने के लिए उन्हें आसानी से पर्याप्त लोहा मिल जाता थे। प्राचीन इतिहास से लेकर आज वर्तमान तक यह बात लागू होती है कि जिसके पास जितने हथियार हैं, वह उतना मजबूत है। मगध के लिए अवंती को ना जीत पाने का भी यही एक बड़ा कारण था क्योंकि मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी लोहे खाद्यान्नों से भरा पड़ा था इसलिए अवंती साम्राज्य भी हथियार के मामले में आत्मनिर्भर था।
मगध की दोनों राजधानी पहली राजगीर और दूसरी पाटलिपुत्र, बहुत ही सोच समझकर बसाया गया था। ये दोनों राजधानी विरोधी सेना के लिए अभेद्य थीं। राजगीर पांच पहाड़ियों के समूह से घिरा हुआ था और उस दौर के लिहाज से बिल्कुल ही अभेद्य था क्योंकि तब किलों पर हमला करने के लिए तोप नहीं हुआ करती थीं।
जब मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया, तब भी उसके स्थान का खास ध्यान रखा गया। पाटलिपुत्र गंगा, पुनपुन और सोन नदी के संगम पर स्थित था। इसके अलावा एक और नदी थी घाघरा। उस जमाने में संचार का कोई दूसरा साधन नहीं था, तो सेना नदियों के रास्ते को फॉलो करके ही आगे बढ़ती थी। इस लिहाज से पटना की स्थिति और अभेद्य थी क्योंकि यह चारों तरफ से नदियों से घिरी हुई थी। गंगा और सोन ने इसे उत्तर और पश्चिम से घेर रखा था जबकि पुनपुन ने इसे दक्षिण और पूर्व से। इस तरह से पाटलिपुत्र एक ऐसा जलदुर्ग बना, जिसे भेदने की कोशिश सालों साल तक नाकाम रही।
खैर, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध को बिंदुसार ने संभाला। बिंदुसार, मौर्य वंश के दूसरे सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, जिन्होंने लगभग 297–273 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। उन्हें 'अमित्रघट' यानी कि शत्रुओं का संहार करने वाला के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार का शासन अपने पिता चंद्रगुप्त और पुत्र अशोक के शासन की तुलना में कम उल्लेखित है। बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित विशाल मौर्य साम्राज्य को बनाए रखा, जो अफगानिस्तान से बंगाल और दक्कन तक फैला था। कुछ स्रोतों के अनुसार उन्होंने दक्षिण भारत में और विस्तार किया, विशेष रूप से दक्कन क्षेत्र में, हालांकि केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से मौर्य नियंत्रण से हमेशा बाहर रहे।
बिंदुसार के शासनकाल के अंत में उत्तराधिकार को लेकर विवाद भी उत्पन्न हुआ। बौद्ध ग्रंथों, जैसे दिव्यावदान, में उल्लेख है कि अशोक ने अपने भाइयों, विशेष रूप से सुसीम को हराकर सिंहासन हासिल किया, जो बिंदुसार के शासनकाल के अंत में दरबार की आंतरिक अस्थिरता को दर्शाता है।
सम्राट अशोक और मौर्य काल का पतन
बिंदुसार के बाद उनके पुत्र अशोक ने मगध की गद्दी संभाली और मगध के इतिहास के सबसे ज़्यादा ख्याति प्राप्त सम्राट बने। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक अपनी उम्र के शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे और गद्दी पर बैठने के लिए उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था। इस बात पर मतांतर है कि भाई 99 थे या नहीं लेकिन इसपर ज़्यादातर इतिहासकार सहमत हैं कि अशोक ने अपने भाइयों को मरवाकर सत्ता हथियाई। कुछ-कुछ अजातशत्रु की ही तरह अशोक की कहानी भी लोगों तक पहुंची एक बड़ी लड़ाई के चलते। अशोक लंबे वक्त से कलिंग फतह करना चाहते थे लेकिन यह काम उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुश्किल निकला। आखिरकार उन्होंने कलिंग को जीत ही लिया लेकिन अशोक के आदेश पर लाखों लोगों की हत्या हुई थी। नदी का रंग लाल हो गया था। यह सब देखकर अशोक ने हिंसा त्याग दी। बौद्ध धर्म अपना लिया।
अशोक का शासन युद्ध से शांति और हिंसा से अहिंसा की ओर एक असाधारण परिवर्तन का प्रतीक है। कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाने के कारण उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को नैतिकता और कल्याणकारी शासन के आधार पर एकजुट किया। अशोक ने 'धम्म' की नीति शुरू की जो नैतिकता, करुणा, अहिंसा और सामाजिक कल्याण पर आधारित थी। यह नीति सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता को बढ़ावा देती थी। अशोक ने अपने शासनकाल में कई शिलालेख बनवाए। जिनमें एक है भारत का राष्ट्रीय चिह्न, अशोक स्तंभ। जो कि बनारस के सारनाथ में है। अशोक के ही प्रयासों ने बौद्ध धर्म को एक विश्व धर्म के रूप में स्थापित किया। जिसका प्रभाव आज भी श्रीलंका, थाईलैंड, जापान और अन्य देशों में देखने को मिलता है।
मगर इन सब चीज़ों का मगध साम्राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ। सेना पर भारी खर्च और नौकरशाही को भारी भुगतान ने मौर्य साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट पैदा कर दिया। लोगों पर लगाए गए विभिन्न करों के बावजूद, इस विशाल ढांचे को बनाए रखना अशोक के लिए मुश्किल हो रहा था। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को बड़े पैमाने पर दान दिया, जिससे उनका शाही खजाना खाली हो गया। अंत में उन खर्चों को पूरा करने के लिए, उन्हें राजकोष में रखी गई सोने की मूर्तियों को पिघलाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
शुंग वंश, कण्व वंश और गुप्त वंश
मौर्यकाल का पतन अशोक के शासनकाल में ही शुरू हो गया था। इसके बाद आगे जो उत्तराधिकारी मिले, उनका नेतृत्व उतना मजबूत नहीं था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या खुद उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। इसके बाद मौर्यकाल का भी अंत हो जाता है और मगध पर अगला शासन शुंग वंश का हुआ और उसके पहले सम्राट बने पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र ने यूनानियों के खिलाफ बहुत युद्ध लड़े। शुंग सम्राटों ने कला एवं संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया लेकिन पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश के उत्तराधिकारी भी उतने मजबूत नहीं रहे और कण्व वंश का उदय हुआ।
कण्व वंश के पहले सम्राट थे वासुदेव कण्व। वह शुंग वंश के आखिरी सम्राट देवभूति के दरबार में मंत्री थे। उन्होंने देवभूति को गद्दी से हटाकर मगध में कण्व का शासन लाया। यह पहला ब्राह्मण वंश था जिसने मगध पर शासन किया। मगर बहुत अल्पकाल के लिए। आंध्र के सातवाहन वंश के राजा ने कण्व वंश के आखिरी सम्राट सुसरमन की हत्या कर मगध पर कण्व वंश के शासन का अंत कर दिया।
इसके बाद कुछ छोटे-मोटे वंश के शासन के बाद फिर बारी आती है, गुप्त वंश की। गुप्त वंश ने मगध पर 320ई से 550ई तक शासन किया। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। मगर वंश को ख्याति दिलाई उनके पोते और घटोतकच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी अर्थात राजाओं का राजा। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारदेवी से शादी करके पड़ोसी राज्य से अपने कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए। यह गठबंधन गुप्तों को बिहार और नेपाल के क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने में सहायक रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने मगध और आसपास के क्षेत्रों (जैसे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश) को अपने नियंत्रण में लिया। उनके शासन ने गुप्त साम्राज्य के लिए एक मज़बूत आधार तैयार किया, जिसे बाद में उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने और विस्तारित किया।
समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठा और प्रभाव भारत के बाहर भी फैला हुआ था। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने शासनकाल में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा था और अपनी इसी वीरता और नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था।
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचा। उन्होंने वैवाहिक गठबंधन और विजयों के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह मध्य भारत में शासन करने वाले वाकाटक के राजकुमार से कराया। राजकुमार की मृत्यु के बाद उनके नाबालिग पुत्र ने सिंहासन संभाला। इस प्रकार प्रभावती ही अप्रत्यक्ष रूप से शासक बनी रहीं। प्रभावती ने अपने पिता चंद्रगुप्त के हितों को ही बढ़ावा दिया। इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय ने मध्य भारत के वाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया, जिससे उन्हें बड़ा लाभ हुआ। इस क्षेत्र में अपने व्यापक प्रभाव के साथ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुशानों से मथुरा पर विजय प्राप्त की। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर कब्जा किया, जो लगभग चार शताब्दी तक शक क्षत्रपों के शासन में रहा था। इस विजय से चंद्रगुप्त को व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी समुद्री तट पर नियंत्रण हासिल हुआ। इससे मालवा और इसके प्रमुख शहर उज्जैन का भी विकास हुआ, जो कि मगध के ही अधीन था।
चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में बनवाया और विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। इस उपाधि को सबसे पहले अवंती के एक राजा ने पश्चिमी भारत के शक क्षत्रप को हराकर ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को पांचवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया से आए हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हालांकि, प्रारंभ में राजा स्कंदगुप्त ने हूणों को रोकने की खूब कोशिश की लेकिन वह नाकाम रहा।
गुप्त वंश के बाद मगध पर लेटर गुप्त वंश यानी कि बाद का गुप्तवंश (6वीं-8वीं सदी), हर्षवर्धन का पुष्यभूति वंश (7वीं सदी) और पाल वंश (8वीं-12वीं सदी) का शासन रहा। इसके बाद पिठापति शासकों का स्थानीय शासन रहा। मगर इसके बाद मगध का केंद्रीय महत्व धीरे-धीरे कम होने लगा और यह क्षेत्र छोटे राज्यों और विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव में आ गया। बौद्ध धर्म और नालंदा जैसे केंद्रों ने इस काल में मगध की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जो तब पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में अलग-अलग देशों के लगभग 10 हजार से ऊपर छात्र और 2000 शिक्षक थे। यह उस जमाने में बहुत ही असाधारण बात थी।
इसके बाद यहां पाल वंश का शासन रहा। पाल वंश के महाराजाओं के खत्म होने के बाद मिथिला में कर्नाट वंश का ज़िक्र मिलता है। बाद में यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन आ गया, जिनके अपने शासक (सूबेदार) होते थे। एक समय मगध के जिस आकार ने सिकंदर को उल्टे पांव लौटा दिया था। वही धीरे-धीरे उसके लिए समस्या बना। लगातार हो रहे हमलों के चलते आखिरकार मगध बिखरने लगा। 12वीं शताब्दी के अंत में एक तुर्क सेनापति- बख्तियार खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया। इसी हमले में और नालंदा सहित कई महत्वपूर्ण स्थान नष्ट कर दिए गए। इस कारण नालंदा का विशाल पुस्तकालय, जिसमें हजारों दुर्लभ पांडुलिपियां थीं, सब जलकर राख हो गया और यह प्राचीन शिक्षा केंद्र हमेशा के लिए नष्ट हो गया।
मुगलों का साम्राज्य
इसके बाद भारत में मुगलों का साम्राज्य स्थापित हुआ। इसके पहले शासक बाबर थे। जिन्होंने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब मुगल साम्राज्य के बड़े शासक हुए। मुगलों ने आज के बिहार और बंगाल सहित भारत के कई हिस्सों पर अपना शासन चलाया। मुगलों ने भारत में 1526 से 1857 तक लगभग 331 साल यहां पर शासन किया।
हालांकि, मुगलों को सबसे बड़ा झटका शेरशाह सूरी ने दिया था। वह भी बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर। शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के ही सासाराम में हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1539 के चौसा युद्ध और 1540 के कन्नौज युद्ध में हराकर मुगलों के साम्राज्य को देश से बाहर फेंक दिया था। मगर शेरशाह की मृत्यु के बाद 1555 में हुमायूं ने एक बार फिर से भारत पर आक्रमण किया। मगर 1556 में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हुमायूं के बेटे अकबर ने बैरम खान की मदद से शेरशाह सूरी के सेनापति हेमू को हराकर फिर से भारत में अपना शासन स्थापित किया।
मुगल इसके बाद धीरे-धीरे मजबूत होते गए लेकिन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक और साम्राज्यवादी संगठन था, जिसने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। कंपनी ने भारत में व्यापार शुरू करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर से 1612 में सूरत में एक व्यापारिक केंद्र यानी की फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। कंपनी ने धीरे-धीरे व्यापार के साथ-साथ राजनीतिक और सैन्य शक्ति हासिल भी हासिल कर लिया। इसने स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ किए और अपनी सशस्त्र सेना बनाई। धीरे-धीरे कंपनी ने व्यापार के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन पर कब्जा करना शुरू कर दिया।
सत्ता संघर्ष के लिए बहुत जल्द ही अंग्रेज और मुगल में टकराव होने शुरू हो गए। 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर कंपनी की सत्ता को मजबूत किया। इसके बाद बंगाल पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके 7 साल बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब को हराकर उत्तर भारत में अपनी स्थिति को और मजबूत किया। इस जीत के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिला। दीवानी मतलब टैक्स कलेक्शन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अगली एक सदी से भी ज़्यादा समय तक भारत पर शासन किया। कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था को अपने हितों के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग खासकर कपड़ा उद्योग को नष्ट किया गया ताकि ब्रिटिश प्रॉडक्ट को बढ़ावा मिले।
कंपनी के शासन के खिलाफ देश में कई विद्रोह हुए, जिनमें सबसे प्रमुख 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह विद्रोह कंपनी के शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष का परिणाम था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों ने भारत का प्रतीकात्मक नेता बनाया। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दिल्ली से निर्वासित कर दिया था। बहादुर शाह जफर जब खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे तो एक अंग्रेज मेजर हडसन ने बहादुर शाह ज़फ़र को गिरफ़्तार कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब बहादुर शाह जफर अंग्रेज़ों के गिरफ़्त में थे तो हडसन ने कहा था- 'दमदमे में दम नहीं, अब ख़ैर मांगो जान की, ऐ ज़फर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की।' मगर बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया, 'गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख़्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की।' अंततः ज़फर गिरफ्तार हुए और उनके दोनों बेटों के सिर कलम हुए। अंग्रेजों ने उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। जहां 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई थी।
ब्रिटिश राज की शुरुआत
अब थोड़ा बिहार पर लौटते हैं। बिहार में जगदीशपुर स्टेट के शासक बाबू वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह गुरिल्ला वॉर में बड़े एक्स्पर्ट थे। इतना कि कई बार अंग्रेज़ों की विशाल सेना भी चकमा खा जाती थी। सिपाही विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने एक बार उनकी नाव पर गोलीबारी शुरू कर दी। जब कुंवर सिंह ने निर्णय लिया कि वह अपनी सेना लेकर वापस लौट जाएं। इसी दौरान अंग्रेज़ों की एक गोली कुंवर सिंह के बाएं हाथ में लगी। उन्होंने संक्रमण का खतरा देखते हुए अपनी तलवार निकाली और अपनी बांह काटकर गंगा में बहा दिया। हालांकि, आगे चलकर उनकी सेना कमजोर पड़ गई और अंग्रेज़ों ने जगदीशपुर एस्टेट पर कब्जा कर लिया। 26 अप्रैल 1858 को अपने गांव में ही वीर कुंवर सिंह की मौत हो गई।
सिपाही विद्रोह में उनकी आक्रामकता का असर पूरे देशभर में हुआ। इस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1858 में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज (British Crown) के अधीन हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट 1858 के तहत भारत में ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। द ईस्ट इंडिया कंपनी को 1874 में पूरी तरह भंग कर दिया गया।
अब भारत पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का शासन था। बंगाल पूरे देश में सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी। इसमें आज का बिहार, झारखंड, ओडिशा, बांग्लादेश सब आते थे। तब अंग्रेज़ों ने देश की राजधानी कलकत्ता में बनाई थी। बिहार की मांग उठने का सबसे बड़ा कारण था कि अंग्रेजों की नज़र में कलकत्ता का महत्व बहुत ज्यादा था और पाटलिपुत्र बस इतिहास में दर्ज होता जा रहा था। बिहार, बंगाल और ओडिशा तीनों एक ही प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आते थे लेकिन प्रशासन ने सिर्फ कलकत्ता को महत्व दिया। इससे बंगाल के लोग अंग्रेजियत के करीब आए। उन्होंने अंग्रेजी सीखी तो सारी प्रशासनिक नौकरियों पर उनका कब्जा बढ़ता गया। इससे बंगालियों का सामाजिक और आर्थिक विकास होना शुरू हो गया। बंगाली पूरे भारतवर्ष में एलीट कहलाने लगे। बंगाली संस्कृति के कारण श्रेष्ठता का भाव था ही। लगातार उपेक्षित महसूस कर रहे बंगाल प्रेसिडेंसी में अन्य क्षेत्र के लोग अलग प्रेसिडेंसी की मांग करने लगे।
1894 में बिहार से सच्चिदानन्द सिन्हा और महेश नारायण ने 'द बिहार टाइम्स' नाम से एक अखबार निकाला और बिहार को अलग प्रेसिडेंसी बनाने की मांग पर जोर देना शुरू किया। इस मांग में वे लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि अगर बिहार का विकास करना है, तो उसका अलग होना बहुत ज़रूरी है। खैर तेज होती इस मांग के बाद बंगाल दो भागों में बंटा जरूर लेकिन अलग बिहार नहीं बना। 16 अक्टूबर 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन कर दिया। हालांकि, कहा यह गया कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह कदम उठाया गया है लेकिन इसकी जड़ में भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करना था। पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहीं पश्चिमी बंगाल हिंदु बहुल। पूर्वी बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश।
खैर बंगाल के दो हिस्सों में बंटने के बाद बिहार के साथ-साथ ओडिशा ने भी अलग प्रेसिडेंसी की मांग शुरू कर दी। क्षेत्रीय नेताओं को यह भरोसा था कि उनके आंदोलन से यह मुमकिन हो सकता है। 1905 के बाद अधिकांश बंगालियों ने अलग बिहार की संभावना को अधिक अनुकूलता से देखना शुरू किया। पटना के सैय्यद अली इमाम, ओडिशा के हसन इमाम, पटना के मजहरुल हक जैसे नेताओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बिहार की तरह ओडिशा में भी अलग प्रेसिडेंसी की मांग बढ़ने लगी।
1908 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र आयोजित हुआ, जहां मुहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग करने की मांग रखी। फिर 1908 में ही दूसरा प्रांत सम्मेलन हुआ बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन यानी कि जमींदार और बिहार के मुस्लिम लीग के नेताओं ने साथ मिलकर पटना में लेफ्टिनेंट-गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर के सामने अलग बिहार प्रेसिडेंसी की मांग की। कुछ ही साल पहले बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम नेताओं के इस गठजोड़ का पूरे बिहार के अंदर सकारात्मक संदेश गया क्योंकि बिहार प्रांत के नेताओं और जनता सिर्फ बिहार के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अलग प्रेसिडेंसी की मांग कर रही थी। यह हिंदू या मुस्लिम नहीं बल्कि पूरे बिहारी समुदाय की मांग थी। आखिर में लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर ने उनकी मांगों पर विचार किया और दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान, ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत के सम्राट के रूप में जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक के अवसर पर बिहार और ओडिशा को बंगाल से अलग किया जाएगा। इस घोषणा को 22 मार्च 1912 को अधिसूचित किया गया और अगले महीने ये दोनों क्षेत्र भारत के नक्शे पर अलग-अलग राज्यों के रूप में उभरे।
और पढ़ें
Copyright ©️ TIF MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED | All Rights Reserved | Developed By TIF Technologies
CONTACT US | PRIVACY POLICY | TERMS OF USE | Sitemap





