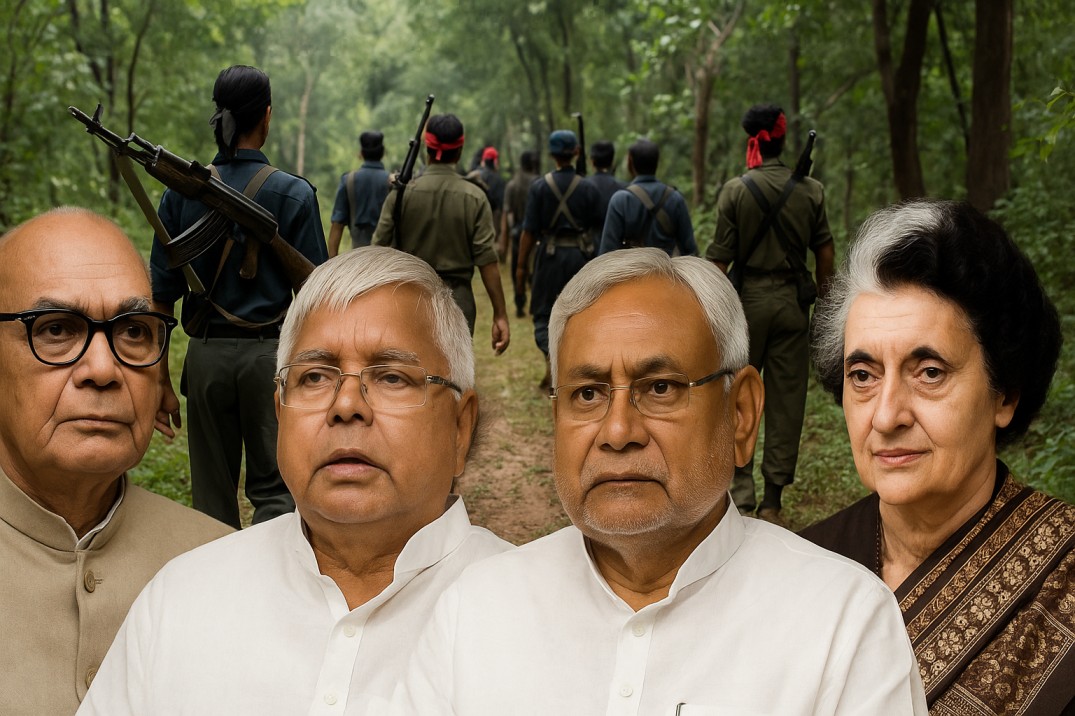साल 1967 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला था। कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए गैर-कांग्रियों ने गलबहियां कर ली थी और इस जुटान की अगुवाई करने रहे थे डॉ. राम मनोहर लोहिया। सूबे के माहौल को भांपते हुए इंदिरा गांधी ने मन बनाया कि समाजवादी धड़े के सबसे चर्चित नेता की सीट पर जाकर चुनौती दी जाए। ताजपुर में रैली हुई। यहां कर्पुरी ठाकुर मैदान में थे लेकिन रैली के दौरान पूरे ताजपुर में इंदिरा ने ऐसा रंग देखा कि उनके चेहरे का रंग बदल गया। इंदिरा आई तो थीं समाजवादियों की धज्जियां उड़ाने लेकिन लौटीं सिर्फ औपचारिक अपील के साथ कि कांग्रेस का साथ दीजिए। इंदिरा जान चुकी थीं कि इस चुनाव का नतीजा क्या होने वाला है। पता तो कर्पूरी और लोहिया को चल चुका था कि समाजवादियों की जीत का ताज सवालों से भरा होगा।
बहरहाल, चुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी लेकिन बहुमत नहीं था। दूसरी ओर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी गैर-कांग्रेसी पार्टी बनी। जिसके साथ कई छोटे-बड़े दल थे और ऐसे दल जो एक साथ मिलकर समाजवादी नेताओं के लिए वैचारिक दलदल बनाने वाले थे लेकिन लोहिया की एक ही जिद्द थी कि चाहे हो जाए बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं बननी चाहिए। उन्होंने एक ही मंच पर वामपंथी धड़े और जनसंघ को ला खड़ा किया। इस मंच को नाम दिया गया- संयुक्त विधायक दल। यह तय माना जा रहे था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी कर्पुरी ठाकुर को ही मिलेगी लेकिन कहानी में ट्विस्ट आना बाकी था। पटना में विधायकों की बैठक बुलाई गई। हर पार्टी का नेता बारी-बारी बोले जा रहा था। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर मुहर लगती जा रही थी। सबसे आख़िर में बोलने वाले थे राजा रामगढ़ कामाख्या नारायण सिंह। कामाख्या सिंह ने वीटो लगा दिया। कर्पूरी के नाम पर सहमत नहीं हुए। दूसरा नाम सुझाया। अपनी ही पार्टी के महामाया प्रसाद सिन्हा। सब चुप हो गए क्योंकि उनके जनक्रांति दल से 30 विधायक चुने गए थे। बात नहीं मानी जाती तो लोहिया के सपने पर पानी फिर जाता और इसी का ख़्याल करके महामाया के नाम को सबने स्वीकार कर लिया। कर्पूरी ठाकुर को डिप्टी का पद मिला।
यह भी पढ़ें- आजादी के बाद का पहला दशक, कैसे जातीय संघर्ष का केंद्र बना बिहार?
पैदा हुआ कांग्रेस को हरा पाने का भरोसा
ख़बर राममनोहर लोहिया तक पहुंची। एक ही वक़्त में खुशी और निराशा दोनों हाथ लगी। बिहार में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनी लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर उसी समुदाय का नेता बैठा था जिससे आने वाले नेताओं ने उस वक़्त तक बिहार में राज किया था। राजपूत-भूमिहार की मोनोपॉली टूट नहीं सकी। लोहिया की नज़र में यह अधूरा समाजवाद था लेकिन अधूरे समाजवाद के उस दौर में दो बड़ी घटनाएं हुईं, जिसने बिहार और एक हद तक पूरे देश की राजनीति को बदलकर रख दिया। पहला, लोहिया के नेतृत्व में यह साबित हुआ कि कांग्रेस को हराया जा सकता है। दूसरा- भारतीय राजनीति में अपने मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवकर संघ की वजह से अछूत बना पड़ा जनसंघ, सियासी अछूतपने से उबरा क्योंकि खुद लोहिया ने संघ के सरसंघचालक एमएस गोलवलकर के साथ हाथ मिलाया और जनसंघ को अपने साथ मंच पर जगह दी।
यह इसी दशक में पड़े बीज की देन है कि बिहार में आज तक कांग्रेस अपने वज़ूद की लड़ाई लड़ रही है। यह इसी दशक में पड़े बीज की देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी अजेय बनी हुई है लेकिन इस दशक में राजनीतिक उथल-पुथल नहीं हो रही थी बल्कि सोशल स्पेक्ट्रम पर - 'राइफल के संग राइफल भिड़ गए, गोली के संग गोली भाय' जैसे गीत गाये जा रहे थे। नारे लग रहे थे बिहार में, हमारा रास्ता, नकस्लबाड़ी का रास्ता। 'नक्सलबाड़ी में बसंत के वज्रनाद' की गूंज बिहार के भोजपुर तक पहुंची और इस गूंज से नक्सल आंदोलन का जन्म हुआ। खूनी खेल हुआ। एक ज़मीन तैयार हुई जिस पर आगे चलकर लाशें बिछने वाली थीं।
राजनीति और कांग्रेस का पतन
2025 में जिस बिहार में कांग्रेस पार्टी अपनी ज़मीन और पैर तलाश रही है, उसी बिहार में एक दौर था जब इस पार्टी का जलवा-जलाल हुआ करता था। एकछत्र राज समझिए। ‘दशक’ सीरीज के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया ही था कि किस तरह पूरे पचास के दशक में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और सिर्फ एक नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए। नाम- श्रीकृष्ण सिन्हा लेकिन फिर आई 31 जनवरी, 1961 की तारीख़। जब श्रीकृष्ण सिन्हा की मृत्यु हो गई। सीएम के पद पर रहते हुए एक स्टालवर्ट नेता की मृत्यु ने पार्टी और शासन तंत्र को हिलाकर रख दिया। तत्कालीन राज्यपाल डॉ. जाकिर हुसैन ने श्रीकृष्ण कैबिनेट के सीनियर मोस्ट मिनिस्टर दीपनारायण सिंह को बुलावा भेजा। दीप नारायण को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई लेकिन उनकी भूमिका एक केयरटेकर सीएम जैसी थी। केयरटेकर सीएम को हटाने के लिए पार्टी विधायकों की गुटबाज़ी हुई और जिस गुट ने इस लड़ाई में जीत हासिल की उसके नेता थे बिनोदानंद झा। जो बिहार के तीसरे सीएम बने। दो सालों के लिए क्योंकि दक्षिण की ज़मीन से आने वाला एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री था, जिसने नेहरू की कान में कुछ मंत्र फूंक दिए थे। नेहरू परेशान थे कि पार्टी की लोकप्रियता कम होती जा रही है तो दक्षिण से चली एक बयार ने उत्तर के एक मुख्यमंत्री को सफाचट कर दिया।
यह भी पढ़ें- राज्य बनने से लेकर दंगों में जलने तक, कैसा था आजादी के पहले का बिहार?
कहानी सुनिए। 1962 में भारत और चीन के बीच जंग हुआ। भारत को इस जंग में हार मिली। संसद से सड़क तक कांग्रेस और केंद्र की नेहरू सरकार पर सवालों की बौछार होने लगी। 1963 में तीन सीटों पर लोकसभा उपचुनाव हुए। तीनों सीटों पर कांग्रेस को शिकस्त झेलनी पड़ी। पार्टी को समझ आ गया कि उसकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। और इन सब के बीच हैदराबाद में पार्टी नेताओं के साथ जवाहरलाल नेहरू मीटिंग करने पहुंचे। मीटिंग में के. कामराज भी मौजूद थे। यह साहब कौन हुए? अभी पता चल जाएगा। कामराज ने नेहरू को सुझाव दिया कि संगठन कमजोर होता जा रहा है। उसकी मरम्मत किए बग़ैर काम नहीं चल पाएगा। नेहरू को यह बात पसंद आई। उन्होंने कामराज से समाधान पूछा। कामराज ने सुझाव दिया कि पार्टी के कद्दावर नेता जो मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर काबिज हैं उन्हें सरकार से हटाकर संगठन में लाया जाए ताकि ये नेता संगठन को मजबूत कर सकें।
कामराज के सुझाव का नतीजा यह हुआ कि केंद्र सरकार से 6 मंत्रियों और 6 राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमंत्री नप गए। जिन मंत्रियों की बलि चढ़ी उनमें लाल बहादुर शास्त्री और जगजीवन राम सरीखे नेताओं का नाम शुमार था। मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में एक नाम बिहार के सीएम का भी था और यह मुख्यमंत्री थे बिनोदानंद झा। कुर्सी ख़ाली हुई तो जगह मिली नेहरू के करीबी केबी सहाय को। सहाय के सामने चुनौती थी बिहार में पार्टी की जीत की स्ट्रीक बनाए रखने की। जो 1952 से चली आ रही थी लेकिन सहाय की सत्ता के खिलाफ आरोपों की ऐसी झड़ियां लगीं कि कांग्रेस पार्टी उससे बच ना सकी।
केबी सहाय और भ्रष्टाचार के आरोप
1967 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए। केबी सहाय की सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों तले दब चुकी थी और ये आरोप खुद केबी सहाय पर भी लगे क्योंकि जिन सहाय के पास 1946 में 600 रुपये थे वह बैलेंस 6 लाख रुपये तक पहुंच चुका था। बतौर सीएम अपना कार्यकाल पूरा करने तक पटना और हजारीबाग सहित कई जगहों पर उनके घर बन गए थे। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को बढ़ावा देने के आरोप सिर्फ सहाय पर ही नहीं लगे बल्कि उनके मंत्रिमंडल में बैठे महेश प्रसाद सिन्हा से लेकर सतेंद्र नारायण सिंह जैसे मठाधीशों पर भी लगे।
यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 1962: कांग्रेस की हैट्रिक, विपक्ष ने दी बदलाव की आहट
इन विवादों के बीच बिहार कांग्रेस को ये अंदाजा लग चुका था कि पहली बार सूबे में उसकी सत्ता जाने वाली है लेकिन केबी सहाय को ये बात तब समझ आई, जब उनके घर में ही एक दिलचस्प वाकया घटा। इस घटना का ज़िक्र इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े पत्रकार संतोष सिंह की किताब Ruled or Misruled में मिलता है। संतोष सिंह लिखते हैं कि केबी सहाय ने पटना के छज्जूबाग स्थित अपने आवास पर अपने ही पोते के मुंह से उनके खिलाफ अपमानजनक चुनावी नारे लगाते सुना। पोता आख़िर क्या नारे लगा रहा था?
गली-गली में शोर है
केबी सहाय चोर है
समझ आता है कि विरोधी गुट के प्रचार की पैठ खुद केबी सहाय के घर तक पहुंच चुकी थी। तिस पर सामाजिक तौर पर पिछड़ी जातियों का उभार भी उस वक्त के सवर्ण डॉमिनेटेड कांग्रेस के लिए चुनौती बनने वाला था। संतोष सिंह अपनी किताब में लिखते हैं, '1966 में, सीएम सहाय ने दुसाध (अनुसूचित जाति) पासवान महासभा की अध्यक्षता करने की इच्छा व्यक्त की थी। पासवानों ने दृढ़ता से कहा कि केवल एक पासवान को ही उनकी बैठक की अध्यक्षता करनी चाहिए। यह शायद पहली बार था जब किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने उच्च जाति के शासन का विरोध किया था।'
सहाय की हार तय थी। हार की पटकथा लिखी जा रही थी और इसमें एक अध्याय पटना के बीएन कॉलेज में लिखा गया लेकिन स्याही से नहीं, खून से। क्या हुआ था बीएन कॉलेज में? स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था क्योंकि फीस बढ़ गई थी। प्रोटेस्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारे लग रहे थे। प्रोटेस्ट के बीच लाठियां चलीं, फिर चलीं गोलियां। Ruled or Misruled किताब में पत्रकार संतोष सिंह लिखते हैं, '5 जनवरी, 1967 को छात्र संघ नेता दीनानाथ पांडेय की हत्या हो गई। आरोप लगे कि दीनानाथ की मौत पुलिस की गोली से हुई है। कायदे से सरकार को इस प्रकरण की जांच करानी चाहिए थी लेकिन जब सहाय की छुट्टी ही तय थी तो क्या होना चाहिए था और क्या हुआ के बीच फासला तो होना ही था। सो हुआ भी।
दोनों सीटों से हारे केबी सहाय
लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपाने वाले सहाय ने घोषणा कर दी कि बीएन कॉलेज में हुई गोलीबारी की कोई जांच नहीं होगी। तिस पर एक घनघोर सियासी इल्जाम भी लगा गए। बोले कि, छात्रों का आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेट था। प्रदर्शन में गुंडे शामिल थे। यह बयान था और सहाय लोगों के निशाने पर चढ़ गए। छात्रों ने आने वाले आम चुनाव में केबी सहाय और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को हराने के लिए अपने खून से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए। नतीजे आए तो शपथ पत्र पर लिखीं बातें मूर्त रूप ले चुकी थीं। चुनाव में केबी सहाय पटना पश्चिम और हजारीबाग से विधानसभा की दोनों सीटें हार गए।
यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 1952: पहले चुनाव में कांग्रेस का जलवा, श्रीकृष्ण बने CM
मुहावरा लोकप्रिय है कि फलां व्यक्ति ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली लेकिन सहाय के कार्यकाल के उत्तरार्द्ध में जिस तरह के फैसले लिए जा रहे थे उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी कुल्हाड़ी बिछाकर कूद रही थी। दूसरी तरफ समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा गठित संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसोपा ने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को ख़ूब उछाला। लोहिया तो पहले ही देशभर में घूम-घूमकर कांग्रेस शासन और नेहरू मॉडल की धज्जियां उड़ा रहे थे। लोहिया ने एक आंदोलन पटना में भी किया था। 9 अगस्त, 1965 की तारीख़ थी। इस दिन केबी सहाय के कंट्रोल वाली पुलिस सरकार की ताबूत में आख़िरी कील ठोंकने वाली थी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लोहिया ने जनसभा को संबोधित किया। उसी रात लोहिया समेत कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारियों ने आग में घी का काम किया। 10 अगस्त को आंदोलन और बड़ा हो गया। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठियों की मार से कर्पूरी ठाकुर, रामानंद तिवारी और चंद्रशेखर सिंह जैसे नेता बुरी तरह घायल हो गए लेकिन पुलिस का इससे भी मन नहीं भरा। प्रसन्न कुमार चौधरी और श्रीकांत अपनी किताब ‘बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम’ में लिखते हैं, '18 जगह पुलिस ने गोलियां चलाईं। संसोपा के अध्यक्ष एसएम जोशी को बिहार में घुसने नहीं दिया गया। राजनारायण पटना जंक्शन से खदेड़ दिए गए। मधु लिमये की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया।'
बिहार में कांग्रेस की हार की शुरुआत
इन सब का नतीजा दो साल बाद आया। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार बिहार की सत्ता से बेदखल हुई। संतोष सिंह लिखते हैं, '1967 का साल कांग्रेस के लिए एक से ज़्यादा मायनों में पहली घंटी बजाने वाला था। संसोपा को 68 सीटें मिली थीं। राष्ट्रीय स्तर पर जनसंघ और सीपीआई ने मिलकर संयुक्त विधायक दल मोर्चा बनाया जिसने आठ राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ़ जीत हासिल की। चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और अजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के। यह सब डॉ. राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में देशव्यापी आंदोलन के कारण संभव हुआ, जो लंबे समय से ओबीसी के प्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठा रहे थे।' बिहार में एसएसपी ने सफलतापूर्वक नारा दिया था- ‘संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ’ लेकिन मार्च 1967 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार के गठन में बिहार ने एक क्रूर, राजनीतिक मजाक देखा। संसोपा, जो कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, को कांग्रेस छोड़कर आए महामाया प्रसाद सिन्हा का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिनके जन क्रांति दल ने सिर्फ 26 सीटें जीती थीं। जब कर्पूरी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय था, तब पार्टी में उनके प्रतिद्वंद्वी रामानंद तिवारी, बीपी मंडल और जगदेव प्रसाद ने कर्पूरी की उम्मीदवारी का विरोध किया। आखिरकार सिन्हा मुख्यमंत्री बने और कर्पूरी उनके डिप्टी। फिर भी कर्पूरी ठाकुर ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा विभाग संभाला।
शिक्षा विभाग के मुखिया बनकर यहां कर्पूरी ठाकुर एक ऐसा काम करने वाले थे जो बिहार के इतिहास में दर्ज होने वाला था। कर्पुरी ठाकुर ने बिहार विधानसभा में छात्रों के लिए स्कूल फीस माफ करने और सबसे महत्वपूर्ण बात मैट्रिक पास होने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव पारित करवाया। भले ही तब एलीट क्लास ने इसे 'कर्पूरी विभाजन' कहकर मजाक बनाया लेकिन इस फैसले ने पिछड़े और दलित वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल-कॉलेजों का दरवाज़ा खोल दिया।
यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 1957: फोर्ड का काम और जोरदार प्रचार, दोबारा जीती कांग्रेस
जिस शिक्षा विभाग से जुड़े एक ऐतिहासिक फैसले ने कर्पूरी ठाकुर को बिहार में लोकप्रिय बना दिया। उसी शिक्षा विभाग से जुड़े एक अदने-से नियुक्ति के मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि महामाया की कुर्सी चली गई। असल बात यह है कि भले ही महामाया प्रसाद सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। घूसखोरी बंद हुई। छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई पर ब्रेक लगा लेकिन महामाया के पास विधायकों की संख्या वाली टैली में भरोसेमंद संख्या नहीं थी। अपनी पार्टी के सिर्फ 26 विधायक थे, बाकी बैसाखी के नोट-बोल्ट। ख़ैर उस कहानी पर आते हैं जिसने महामाया को एक साल भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं रहने दिया।
कैसे गई महामाया सिंह की कुर्सी?
यह कहानी जुड़ी है पटना मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर की नियुक्ति से। प्रोफेसर दलित समुदाय से आते थे और यह वह दौर था जब बिहार की राजनीति में अभी-अभी ही इस समुदाय ने सीना तानना शुरू किया था। प्रोफेसर की नियुक्ति का मामला लेकर सीएम के दफ्तर विधायकों की टोली के साथ पहुंचा एक पहली बार का विधायक। नाम- सतीश प्रसाद सिंह। विधानसभा क्षेत्र- परबत्ता। पार्टी- संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। वही संसोपा जिसके सर्मथन से महामाया प्रसाद सरकार चला रहे थे। पहली बार के ही विधायक ने अपनी ठसक दिखाई और दलित प्रोफेसर की नियुक्ति के मसले पर सरकार को घेर लिया लेकिन घेरेबंदी का मकसद पूरा होने से पहले यहां कहानी में एक और क़िरदार की एंट्री होती। यह बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। वही मंडल आयोग वाले बीपी मंडल। यह नाम याद रखिएगा, ख़ूब चर्चा होगी इनपर।
ख़ैर। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सतीश प्रसाद सिंह के साथ दो नेताओं ने ख़ूब बतकुच्चन किया। पहले पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके केबी सहाय और दूसरे बीपी मंडल। केबी सहाय ने सतीश सिंह को सीधा ऑफर दिया कि अगर वह 25-30 विधायकों को संसोपा से तोड़ लें तो कांग्रेस के 155 विधायक उन्हें समर्थन कर देंगे और इस तरह सीएम की कुर्सी उनकी हो जाएगी। दूसरी तरफ बीपी मंडल थे जो संसोपा के नेता राममनोहर लोहिया से उखड़े हुए थे। लोहिया पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि वह मंडल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मंडल और सतीश की जोड़ी बैठ गई और एक योजना बनी। योजना यह कि सतीश प्रसाद सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। फ़िर राज्यपाल से बीपी मंडल को MLC नियुक्त करने के लिए अनुशंसा करेंगे ताकि मंडल को सरकार में एंट्री मिले और फिर उन्हें सीएम बनाया जा सके। सब कुछ प्लान के मुताबिक़ हुआ। तारीख़ आई 27 जनवरी, 1968। शाम के साढ़े सात बज रहे थे। राजभवन में सतीश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
एक तरफ पद की शपथ ली गई। दूसरी तरफ एक नेता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह विधान परिषद के मनोनीत सदस्य परमानंद सहाय थे। जिन्होंने बीपी मंडल के लिए सीट ख़ाली की। सीट ख़ाली हुई तो सतीश प्रसाद सिंह ने राज्यपाल से इस पर बीपी मंडल के मनोनयन की अनुशंसा की और इस तरह बीपी मंडल MLC हुए। जो लक्ष्य था वहां पहुंचने के लिए मंडल को सिर्फ एक हफ़्ते का इंतज़ार करना पड़ा। 3 फरवरी के दिन तत्कालीन राज्यपाल एन. कानूनगोई ने बीपी मंडल को सरकार बनाने का न्योता भेजा। 5 फरवरी को बीपी मंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली।
मंडल की ताजपोशी और विदाई
पटना की सड़कों पर मंडल के शपथ ग्रहण की गूंज अभी शांत भी नहीं पड़ी थी कि उनकी विदाई की पटकथा लिखी जाने लगी क्योंकि आख़िरकार मंडल सरकार जिस बैसाखी पर चल रही थी उसका नाम कांग्रेस था। वह कांग्रेस जिसमें हाथ की उंगलियों से ज्यादा गुट बने हुए थे। तो ऐंटी केबी सहाय गुट इस बात को पचा नहीं पाया कि सहाय के कहने पर वह दूसरी पार्टी के किसी नेता की सरकार चलवा रहे हैं। कामराज प्लान में निपट चुके और सहाय के विरोधी बिनोदानंद झा ने अगुवाई की। विधायकों की एक टोली ने पार्टी तोड़ दी। नई पार्टी की नींव पड़ी। नाम रखा गया लोकतांत्रिक कांग्रेस। यादव बिरादरी से आने वाले बीपी मंडल की सरकार गिर गई। लोकतांत्रिक कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों के समर्थन से सरकार बना लिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पहली बार अनुसूचित जाति से आने वाले एक नेता भोला पासवान शास्त्री को मिली।
दलित समुदाय का एक नेता सूबे की सत्ता के शीर्ष पर स्थापित हुआ। पॉलिटिकल नैरेटिव तैयार हुआ। मंडल हटे तो पासवान आए लेकिन भोला पासवान शास्त्री सत्ता की खटिया यानी चारपाई पर बैठे थे। ऐसी खटिया जिसकी पैर से लेकर रस्सी तक अलग-अलग दिशाओं से आई थीं। मिज़ाज और राजनीति भी बिल्कुल अलग। इसी में एक पैर का नाम था जनक्रांति दल। इस पार्टी के मुखिया थे कामाख्या नारायण सिंह। जमींदार थे और केस लड़ रहे थे बिहार सरकार के खिलाफ। जमींदारी का मसला था। अब वह सरकार में एक प्रमुख साझेदार थे। कामाख्या सिंह ने अर्जी लगाई की जमींदारी वाले केस में उनके समर्थन से चल रही सरकार पीछे हट जाए लेकिन समर्थन तो समाजवादी गुट का भी था ही। जो जमींदारी के मुद्दे पर एक इंच पीछे हटने की बात भर से तुनक जाते थे।
बिहार में बुजुर्ग कहते हैं, ‘जोतल खेत में दौड़ल सभका बस के बात नइखे।’ और बिहार की राजनीतिक खेत तो उस दौर में कई राउंड जोती जा चुकी थी। यहां तो चलने के लिए भी ऊंट का खुर होना चाहिए था। जो कि भोला पासवान शास्त्री और उनके किंगमेकर बिनोदानंद झा के पास नहीं था। तो खेत में पैर फंसे और सरकार औंधे मुंह गिर गई। 29 जून, 1969 की तारीख़ थी। जब भोला पासवान शास्त्री के नाम के आगे भी पूर्व सीएम का तमगा लग गया।
भोला पासवान का एक और कार्यकाल
सरकार तो गिरी लेकिन इस बार कोई नहीं पहुंचा सरकार बनाने के लिए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। बिहार साठ के दशक के अंत की दहलीज पर खड़ा था और हम खड़े हैं इस दशक की सियासी उठा-पटक की कहानियों के आख़िर पड़ाव पर। जहां 8 महीनों के राष्ट्रपति शासन के बाद बिहार में मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव में विपक्ष खेत में बिखरे ढेला-माटी की तरह ही बिखरा हुआ था लेकिन कांग्रेस पार्टी डंडेर पर जड़ जमाए हुए थी। चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। 118 सीटें थीं उसके पास लेकिन पूर्ण बहुमत से काफ़ी कम। नयाग्राम से विधायक चुनकर आए थे कांग्रेस नेता हरिहर सिंह। उन्होंने पार्टी के निर्देश पर कुछ और दलों के विधायकों को साधा और सरकार बना ली। जिन दलों को साधा था उसमें कामाख्या नारायण सिंह की पार्टी भी थी लेकिन पार्टी का नाम जनक्रांति दल से जनता दल हो चुका था। कामाख्या सिंह को हरिहर सिंह की सरकार में मंत्री पद मिला। इस पर दूसरे सहयोगी बिदक गए। वजह फिर से वही जमींदारी थी। कामाख्या सिंह जैसे जमींदार का मंत्री बनना शोषित दल को रास नहीं आया। उन्होंने विरोध किया और इसी उठा-पटक के बीच हरिहर सिंह की सरकार लड़खड़ा कर गिर गई। फरवरी, 1969 से जून, 1969 तक ही सरकार चला पाए थे। राष्ट्रपति शासन से पहले सीएम रहे लोकतांत्रिक कांग्रेस वाले भोला पासवान शास्त्री ने फिर चारपाई की बुनाई की और सीएम बन गए लेकिन सिर्फ 12 दिन के लिए। हुआ यह कि भोला पासवान की चारपाई में इस बार एक पैर जनसंघ का था। जिसके पास 34 विधायक थे। सरकार बनाने का दावा पेश हो गया। शपथ ग्रहण भी हो गया लेकिन विधानसभा में जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो जनसंघ ने हाथ पीछे कर लिया और यह दूसरा मौका था जब भोला पासवान शास्त्री ने कुर्सी गंवाई तो सूबे में राष्ट्रपति शासन लग गया। 16 फरवरी, 1970 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उसके बाद क्या हुआ? जवाब ‘दशक’ सीरीज के तीसरे एपिसोड में मिलेगा। जहां हम सुनाएंगे आपको सत्तर के दशक की कहानी। क्योंकि यहां साठ के दशक का होता है अंत।
साठ के दशक में बिहार की राजनीति का चैप्टर क्लोज हो चुका है तो लगे हाथ यहीं कुछ रिमार्क नोट कर लेते हैं। इसी दशक में बिहार ने पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार देखी। अगुवाई राममनोहर लोहिया कर रहे थे। लोहिया कांग्रेस को हटाने के लिए हर तरकीब अपना रहे थे। उन्हें पता था कि वैचारिकी के स्पेक्ट्रम पर एकदम उलट जनसंघ और वाम दलों के साथ मिलकर सरकार चला पाना नामुमकिन था लेकिन लोहिया यह मानते थे कि प्राथमिकता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना है और इसके लिए चाहे जो करना पड़ा जाए। 'चाहे जो करना पड़े', यह एक ऐसी स्थिति है जो बहुत आसानी से अपने साथ अस्थिरता लेकर आती है और इसलिए यह बिहार की राजनीति की अस्थिरता का आरंभ था। ऐसा आरंभ जो पहले दिन से चरम की स्थिति तक पहुंच गया। कभी कोई 7 महीने के लिए सीएम बना तो कभी कोई 7 दिन के लिए। सीएम की कुर्सी और सूबे की सरकार मानो विजय राज के उस मीम की तरह हो गया था, जिसमें विजय राज कहते हैं, 'सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा।' बिल्कुल इसी सूत्र पर चलते हुए साठ के दशक में जो मठाधीश नेता जिसे चाह रहा था उसे सीएम बना दे रहा था। वैचारिकी की राजनीति के दंभ से भरे इसी दशक में कभी राम-वाम एक साथ दिख जाते थे तो कभी जमींदारों की पार्टी, समाजवादियों के साथ। गुटबाजियों के इस दौर में हर बार आम खाने वाले क़िरदार भले बदल रहे थे लेकिन जिनकी गुठली सूख रही थी वह क़िरदार सिर्फ एक ही था और यह थी कांग्रेस पार्टी। हर गुटबाजी कुल्हाड़ी की काट की तरह बरगद सरीखे कांग्रेस की जड़ पर लग रही थी और यह काट ही होती चली गई। कांग्रेस का पत्ता साफ़ ही होते गया और इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी शर्ट-पैंट की तरह बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगी लेकिन यह सब होगा अगले दशक में।
लालू और नीतीश की एंट्री
फिलहाल तो आप इसी दशक में पॉलिटिक्स की ABCD सीख रहे दो नेताओं की कहानी सुनिए। ऐसे नेता जिन्होंने बाद के दशकों में बिहार पर एकछत्र राज किया। ये दोनों यूनिवर्सिटी के दिनों से सीनियर-जूनियर थे। फिर दोस्त बने लेकिन कई बार एक-दूसरे के खिलाफ़ ही शतरंज की चाल चलते भी दिखे। पहले बात सीनियर की।
साल 1973। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव होने वाला था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समाजवादी युवजन सभा ने गठबंधन कर लिया। चुनाव हुए और ABVP-SYS गठबंधन ने छात्र संघ चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया। सुशील कुमार मोदी जेनरल सेक्रेटरी बने। रविशंकर प्रसाद ज्वाइंट सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट बना एक ठेठ देहाती लहज़े का युवा छात्र नेता। वही नेता जो 1971 के छात्र संघ चुनाव में हार गया था क्योंकि तब पटना यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे थे- 'राइफल बुलेट जिंदाबाद'। यह एक सांकेतिक नारा था, जिसमें जाति की दबंगई थी। भूमिहारों और राजपूतों के वर्चस्व का नारा और इसी नारे के लपेटे में वह नेता भी आ गया था। एक युवा नेता जिसे लोहा सिंह का मिथकीय क़िरदार हीरो लगता था। लोहा सिंह जो कहा करता था, 'काठ के बंदूक से लोहे का संदूक तोड़ देता हूं।' नेता का नाम- लालू प्रसाद यादव। वही लालू जिनका बिहार की राजनीति में वर्चस्व का एक पूरा दौर रहा है। लालू प्रसाद यादव भी सियासी फलक पर पहली बार इसी साठ के दशक में टिमटिमाते दिखे। राजनीति की नर्सरी यानी छात्रसंघ में।
गोपालगंज के फुलवरिया गांव से पटना पढ़ाई के लिए आए लालू प्रसाद यादव की कहानी इसी दशक में शुरू होती है। गांव के भदेस मुहावरों से लदी भाषा बोलने में माहिर लालू प्रसाद यादव 1969 में समाजवादी युवजन सभा के ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए। संतोष सिंह अपनी किताब 'Ruled or Misruled' में लिखते हैं, 'संभवतः यह पहला मौका था जब किसी ने लालू का नाम सुना।' इसी वक़्त में लालू के नाम से जुड़ा एक दिलचस्प क़िस्सा भी है। इस वक़्त तक लालू यादव अंग्रेजी में नाम लिखते हुए LALLU लिखते थे लेकिन कुछ साथियों ने बताया कि लोग इस स्पेलिंग की वजह से उन्हें लल्लू यानी मूर्ख कहकर बुलाते हैं। इसके बाद उन्होंने अपने नाम के बीच से एक L हटाया और अंग्रेज़ी में नाम लिखा गया- LALU PRASAD YADAV।
लालू जब यह सब कर रहे थे, उसी वक़्त में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक लड़का पढ़ाई कर रहा था। जिसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर सरीखे नेताओं की संगत में हो रही थी। इस लड़के को दुनिया आज नीतीश कुमार के नाम से जानती है लेकिन नीतीश, नीतीश तब बने जब 1974 का साल आया। बिहार के छात्र गोलबंद हुए। जेपी ने मोर्चा संभाला और बिहार में एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसने देश की राजनीति को अपने तईं बदलकर रख दिया।
यहां तो अब बात होगी एक और आंदोलन की। ऐसा आंदोलन जिसने पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी से प्रेरणा हासिल की। नतीजा यह हुआ कि पहले पूरा भोजपुर रीजन और बिहार का एक बड़ा हिस्सा इस आंदोलन की चपेट में आ गया। बात बिहार में नक्सल आंदोलन के जन्म की।
नक्सल मूवमेंट और जातीय हिंसा
तारीख़ 5 जुलाई, 1967। चीन में छपने वाली एक कम्युनिस्ट अख़बार ने भारत से जुड़ी एक ख़बर छापी। हेडलाइन थी ‘Spring Thunder Over India’। हिंदी तर्जुमा- ‘भारत पर वसंत का वज्रनाद’। क्या हुआ था भारत में? और क्या थी यह ख़बर जिसे चीन के कम्यूनिस्ट अख़बार ने वसंत का वज्रनाद करार दिया? और इस कहानी का बिहार से क्या नाता है? इसे समझने के लिए उस राज्य में प्रवेश करना होगा जो साल 1912 में बिहार से अलग होकर वजूद में आया। सूबे का नाम पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है नक्सलबाड़ी। जहां 1967 में कम्युनिस्ट दस्ते ने सशस्त्र संघर्ष का बिगुल फूंका। जिस दौर में बिहार हर बदलते मौसम के साथ एक नया मुख्यमंत्री देख रहा था, उसी दौर में नक्सलबाड़ी के आदिवासी किसान चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे कम्युनिस्ट नेताओं के नेतृत्व में जमींदारों और पुलिस से भिड़ गए। 52 दिनों तक विद्रोह चला। इस आंदोलन को इतिहास के पन्नों ने नक्सलबाड़ी आंदोलन के नाम से याद रखा है।
नक्सलबाड़ी में लगी आग की धाह बिहार तक पहुंची। भोजपुर में कुछ युवा थे जिनके ज़ेहन में नक्सलबाड़ी मॉडल घर कर गया था लेकिन यह घर यूं ही नहीं बना था। बल्कि इस नींव तब पड़ी जब एकवारी गांव में भूमिहारों ने दलित समुदाय के एक युवक को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया। संतोष सिंह की किताब 'Ruled or Misruled' में क़िस्सा दर्ज है। 1967 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा था। जगदीश महतो उर्फ जगदीश मास्टर एकवारी गांव के मुखिया और CPI मेंबर रामनरेश दुसाध के करीब आ गए थे। चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राजदेव राम को जगदीश महतो के दोस्त रामनरेश के खिलाफ़ आरक्षित सहार सीट से खड़ा किया गया था। 17 फरवरी, 1967 की तारीख, वोटिंग का दिन। जगदीश महतो पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालने पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक भूमिहार समुदाय के व्यक्ति ने राजदेव राम के पक्ष में पोलिंग बूथ पर धांधली की है। एचडी जैन कॉलेज में साइंस पढ़ाने वाले जगदीश महतो ने दबंग ऊंची जाति के लोगों को धांधली करने से रोका। जगदीश अकेले थे। भूमिहारों ने उन्हें पकड़ लिया बलभर पीटा। इतना मारा की जगदीश महतो पांच महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे। जब अस्पताल से लौटे तो ‘वसंत के वज्रनाद’ की गूंज उनकी कानों में गूंजने लगी थी।
जो गूंज कानों में भरे थे वह दीवारों पर उतर गए और 1969 आते-आते तो आरा की दीवारें नक्सली नारों से पट गईं। तमाम नारों के बीच एक नारा 14 अप्रैल, 1970 को लगा। इस दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती थी। जगदीश महतो और रामेश्वर अहीर के नेतृत्व में रैली निकली। नारा लगा- 'हरिजनिस्तान लड़कर लेंगे।'
बिहार में नक्सलवाद का यह आरंभ था और इस वक़्त में सिर्फ नारे नहीं गूंज रहे थे। बल्कि हथियार भी शोर मचाने लगे थे। दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, हजारीबाग जैसे इलाकों में सशस्त्र किसान संघर्ष की कोशिशें शुरू हो गईं। गुरिल्ला युद्ध छिड़ गया। बानगी देखिए। अप्रैल, 1968 का महीना। मुसहरी प्रखंड का गंगापुर गांव। कुछ बेदखल बटाईदारों ने एक जमींदार की जमीन पर कब्जा कर लिया। किसानों के बीच ‘फसल कब्ज़ा करो और ज़मीन कब्ज़ा करो’ का नारा गूंजने लगा। गंगापुर के किसान हथियार लेकर अपने घरों से निकलने लगे और ज़बरदस्ती ज़मींदारों की ज़मीन से अरहर की खड़ी फसल काटने लगे। जमींदारों और किसानों के बीच अप्रैल की तपती गर्मी में ख़ूब लड़ाइयां लड़ी गईं।
जमींदारों पर खूब हुए हमले
लड़ाइयों का दूसरा किस्त खुला अगस्त महीने में। आज़ादी का दिन यानी 15 अगस्त की तारीख। नक्सलियों के नेतृत्व में किसानों ने मुशहरी गांव में सशस्त्र रैली निकाली। यह सीधे तौर पर जमींदारों को चुनौती थी। रैली में 'नक्सलबाड़ी जिंदाबाद' से लेकर 'नक्सलबाड़ी का रास्ता, हमारा रास्ता' तक के नारे लग रहे थे। यह रैली गांव के जमींदारों को चुभ गई। पुलिस के सहयोग से 5000 लोगों की रैली घेर ली गई और अंत में 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नतीजतन गुस्सा भड़क गया। गांव के किसानों ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। जमींदारों पर हमले शुरू हुए। इन हमलों में 18 लोगों की हत्या की गई। जो या तो जमींदार थे या उनके एजेंट। किसानों ने जमींदारों के घर में रखे खेत-खलिहान के दस्तावेजों में आग लगा दी।
सेंट्रल बिहार रीजन में ऐसे छोटे-बड़े कई हमले हुए। जमकर रक्तपात हुआ। प्रसन्न चौधरी और श्रीकांत की किताब ‘बिहार में सामाजिक परिवर्तन के आयाम’ से एक आंकड़ा मिलता है। 1970 के बरस में जनवरी से अगस्त के बीच क़रीब 30 मर्डर हुए। नक्सली गतिविधि की वजह से मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिंहभूम, चंपारण, जमशेदपुर, पटना, रांची, गया, सहरसा और हजारीबाग में 954 लोग अरेस्ट किए गए लेकिन अपनी पैदाइश के साथ ही बिहार में नक्सली आंदोलन गहरे तौर पर पैर जमाता दिखा।
आल्हा गाए जाने लगे-
राइफल के संग राइफल भिड़ गए
गोली के संग गोली भाय
गांव-गांव को चवरी कर दो
हर थाने को करो सहार
जहां का बच्चा-लड़ता
बूढ़ा हाथ धरे हथियार।
यह ऐलानिया गीत था कि बिहार में वर्ग संघर्ष अपने चरम पर पहुंचने वाला है। इसकी दो वजहें थीं। एक दो ज़मींदारों के खिलाफ़ आक्रोश। दूसरी वजह कम्युनिस्ट पार्टी। जगदीश महतो और उनके साथी रामनरेश बिहार में संगठित तौर पर सशस्त्र संघर्ष छेड़ना चाहते थे। नक्सलबाड़ी की ही तरह और इसके लिए उन्हें पार्टी से संपर्क करना ज़रूरी। संपर्क नहीं हो पा रहा था। ऐसे में दोनों को लगा कि शायद वर्ग संघर्ष छेड़ने पर ही पार्टी से संपर्क हो पाएगा। नतीजा यह हुआ कि बिहार में नक्सली आंदोलन के इतिहास के शुरुआती पन्नों पर एक थाने का नाम दर्ज हो गया- सहार। इसी सहार का ज़िक्र थोड़ी देर पहले सुनाई एक गीत में भी आया था। क्या हुआ था सहार में?
जगदीश मास्टर की हत्या
नक्सली दस्ता एक प्लानिंग के तहत भोजपुर जिले के सहार थाने के एकबारी गांव में धमक पड़ा। इस गांव में जमींदारों का एक लठैत हुआ करता था- शिवपूजन सिंह। दस्ते ने हमला किया और शिवपूजन की हत्या कर दी। लाश सोन के किनारे रख दी। मामला खुला तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जगदीश मास्टर और रामेश्वर समेत उनके कई साथियों को अभियुक्त बनाया गया लेकिन हमले रुके नहीं। एकबारी गांव के ही जगदीश सिंह कुछ दिनों बाद मार दिए गए। फिर दुधेश्वर सिंह नाम के जमींदार पर भी हमला हुआ लेकिन वह बच गए। एक के बाद एक हुए बड़े हमलों के बाद जगदीश और रामेश्वर कोलकाता रवाना हुए और आख़िरकार पार्टी से उनका संपर्क हुआ। नतीजतन फरवरी, 1972 में भोजपुर में पार्टी इकाई की स्थापना हुई।
हालांकि, पार्टी इकाई बनने के कुछ ही महीनों बाद बिहिया गांव में उनकी हत्या कर दी गई। संतोष सिंह अपनी किताब में लिखते हैं, 'एकवारी के महतो समुदाय को आज भी यह बात कचोटती है कि किस तरह जगदीश मास्टर को उनके ही लोगों ने ग़लती से मार डाला।' 10 दिसंबर, 1972 की बात है। इस दिन मास्टर का जन्मदिन था। 37 साल की उम्र पूरी हुई थी। उन्होंने अपने दस्ते के साथ हरि सिंह नाम के जमींदार पर हमला कर दिया। नाकाम हुए तो छिपने के लिए भाग रहे थे। भागने के दौरान वह कुछ ट्रक ड्राइवर्स के हाथ लग गए। ड्राइवर्स को लगा कि वह जिस चोर की तलाश कर रहे थे, ये वही शख्स है। उन्होंने जगदीश को लाठी-डंडों से पीटना शुरू कर दिया। मास्टर अपनी पहचान बताने की कोशिश करते रहे लेकिन ड्राइवर नहीं रुके। जगदीश महतो की मौत हो गई।
भोजपुर में नक्सलियों का एक बड़ा लीडर मारा गया लेकिन नक्सली दस्ता रुका नहीं। वह लगातार जमींदारों पर हमले करता रहा। हमले का बीड़ा उठाया था जगदीश मास्टर के कॉमरेड गणेशी दुसाध ने। जो गुरिल्ला युद्ध में पारंगत हो चुका था।
न्यूटन का नियम है- हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब भोजपुर रीजन में लाल दस्ते की दहशत फैलने लगी और जमींदारों के सर्वाइवल का सवाल उठ खड़ा हुआ तो हमला दूसरी तरफ से शुरू हुआ लेकिन जमींदारों के साथ राज्य का पुलिस तंत्र लगा हुआ था। पुलिस ने इस क्षेत्र में नक्सलियों को खत्म करने का अभियान छेड़ दिया। निशाने पर सबसे पहले गणेशी दुसाध का ही नाम था।
6 मई, 1973 की तारीख़। चवरी गांव में पुलिस ने नक्सलियों को घेर लिया। दोनों तरफ से गोलियां चलीं लेकिन गुरिल्ला लड़ाके ख़ुद को बचा नहीं सके। पुलिसिया अभियान में गणेशी दुसाध के साथ-साथ बालकेश्वर राम, लालमोहर दुसाध और दीनानाथ साव मारे गए। ऐसे ही एक के बाद एक कई गांवों में पुलिस और नक्सलियों के बीच भिड़ंत हुई। 12 घंटे से लेकर 65 घंटे तक के मुठभेड़ इतिहास में दर्ज हुए। एक-एक कर जगदीश महतो के साथी दम तोड़ते गए और भोजपुर में कुछ वक़्त के लिए नक्सलियों का सशस्त्र संघर्ष ठहर गया।
यह एक तूफ़ान के पहले की शांति थी और यह तूफ़ान भोजपुर की सीमाओं में नहीं उठना था बल्कि पटना से शुरू होकर पूरे देश में फैलने वाला था। एक आंदोलन जिसके गर्भ से बिहार को ऐसे नेता मिलने वाले थे जिनके हाथ में बिहार की कमान दशकों तक रहने वाली थी। इस कहानी में जयप्रकाश नारायण की एंट्री होने वाली है। संपूर्ण क्रांति का नारा गूंजने वाला है। जेपी के दो शागिर्द- लालू और नीतीश फलक पर दिखने वाले हैं और इन सब के बीच आएंगी देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। जो राष्ट्रपति के हवाले से एक ऐलान करेंगी और पूरा देश किसी कारागार की मानिंद काल-कोठरी में तब्दील हो जाएगा। यानी… आपातकाल।