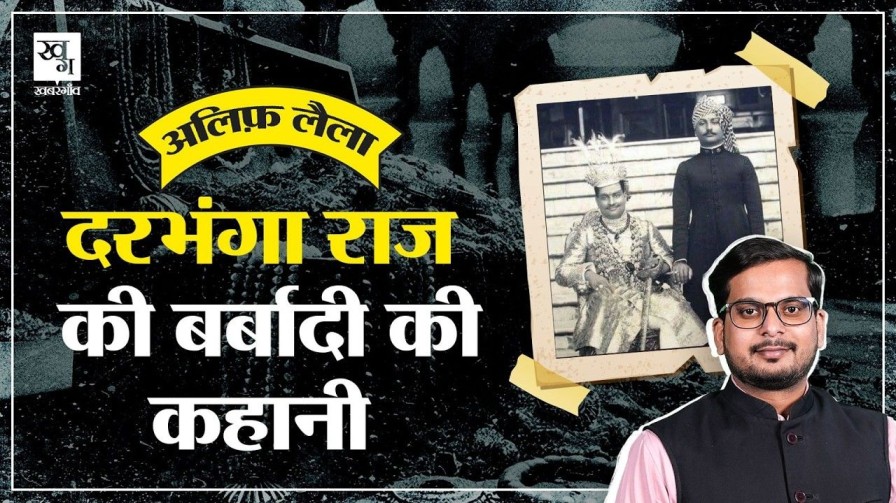एक बार की बात है। मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में एक काज़ी ने शर्त रखी। उन्होंने कहा, 'मैं हिंदू दर्शन पर डिबेट करना चाहता हूं। है कोई जो मुझसे मुकाबला कर सके?' अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल। बीरबल ने तब महेश ठाकुर का नाम सुझाया। महेश ठाकुर, जो उन दिनों गढ़ मंडल में दलपतिशाह के दरबार में पुरोहित हुआ करते थे, उन्हें फतेहपुर सीकरी बुलवाया गया। दरबार में बहस शुरू हुई। महेश ठाकुर एक के बाद एक सवालों का जवाब देते रहे। बहस के अंत में अकबर इतने खुश हुए कि न सिर्फ महेश ठाकुर को विजयी घोषित किया बल्कि अपने साम्राज्य में एक बड़े इलाके का चौधरी और कानूनगो नियुक्त कर दिया। उत्तरी बिहार में मिथिला वाले हिस्से में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था। इसे सरकार तिरहुत कहते थे। इस पूरे इलाके की जिम्मेदारी महेश ठाकुर को मिल गई।
एक साधारण पुरोहित की जीत से शुरू हुई ये कहानी आगे जाकर तब्दील हुई भारत के सबसे अमीर राजघरानों में। जमींदारों का एक ऐसा खानदान, जो 10 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन के मालिक थे। जिसके महाराज, आजादी के वक्त भारतीय अमीरों की गिनती में तीसरे नंबर पर आते थे। ये कहानी है राज दरभंगा की।
मैथिल ब्राह्मणों का एक परिवार भारत की सबसे ताकतवर जमींदारी में कैसे तब्दील हुआ? राज दरभंगा का अंत कैसे हुआ? किस चीज के डर ने दरभंगा के महाराज को कांग्रेस में शामिल होने से रोका? फ्रांस की आखिरी रानी का हार दरभंगा के खजाने में कैसे पहुंचा? कैसे हुई दरभंगा के खजाने की बंदरबांट? कहां गायब हो गया दरभंगा का खजाना?
यह भी पढ़ें- युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल फायदेमंद या अपना नुकसान, इतिहास से समझिए
दरभंगा राज की कहानियां
दरभंगा राज की शुरुआत का जो किस्सा हमने शुरू में सुनाया, वह इकलौता नहीं है। एक कहानी है कि महेश ठाकुर के शिष्य रघुनंदन झा अकबर के दरबार में गए थे। एक दिन उन्होंने देखा कि सम्राट के शिविर के ऊपर एक पेड़ की डाल लटकी है। रघुनंदन ने भविष्यवाणी की कि बिजली गिरेगी और वह पेड़ नष्ट हो जाएगा। सम्राट के कहने पर शिविर को सेफ जगह ले जाया गया। बाद में सच में तूफ़ान आया और पेड़ पर बिजली गिर गई।
अकबर इस भविष्यवाणी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रघुनंदन झा को तिरहुत के राजस्व का दो प्रतिशत देने का वचन दे दिया लेकिन गुरु के प्रति अपनी वफादारी दिखाते हुए रघुनंदन ने यह इनाम अपने गुरु महेश ठाकुर के लिए मांग लिया। इस प्रकार महेश ठाकुर तिरहुत के चौधरी और क़ानूनगो बन गए।
दरभंगा राज से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं। किस्सों से इतर हालांकि यदि धरातल पर आएं तो असली बात ये थी कि तुग़लक़ वंश के अंत के बाद से ही बिहार का इलाका छोटी छोटी लड़ाइयों का गढ़ बना हुआ था। तराई का यह इलाका खेती के हिसाब से अनुकूल था। खूब उगाई होती थी। लेकिन बिना एक सेन्ट्रल अथॉरिटी से आप टैक्स कैसे वसूलते?
यह भी पढ़ें- 300 साल पहले भी औरंगजेब की कब्र पर हुई थी राजनीति, पढ़िए पूरी कहानी
लिहाजा अकबर ने इस इलाके पर अपना कंट्रोल जमाया और महेश ठाकुर को टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी दे दी। महेश ठाकुर के बाद ये जिम्मेदारी मिली उनके बेटे गोपाल ठाकुर को। गोपाल ठाकुर के टाइम में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सर्वे हुआ। इस सर्वे के बाद पहली बार तिरहुत की कमाई का पता चला। सर्वे के बाद तय हुआ कि तिरहुत को हर साल 11 लाख 63 हज़ार रुपये टैक्स चुकाना होगा।
हेमांगद की कहानी
किस्सा है कि एक बार टैक्स चुकाने में देरी हो गई। अकबर ने गोपाल ठाकुर को दिल्ली तलब किया। गोपाल ठाकुर ने अपने पुत्र हेमांगद ठाकुर को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा। पूछताछ के दौरान हेमांगद ने बताया कि स्थानीय विद्रोह के कारण वह समय पर राजस्व नहीं चुका पाए थे। हेमांगद ने बादशाह अकबर से कुछ वक्त की मोहलत मांगी लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया। हेमांगद जिनका परिवार ज्योतिष जानता था, उन्होंने अकबर को मनाने का वही तरीका अपनाया जो कभी उनके दादा ने अपनाया था।
हुआ यूं कि हेमांगद जब कैद में थे। उनके पास कलम दवात तो थी नहीं, लिहाजा उन्होंने कोयलों के टुकड़ों से जेल की फर्श पर कुछ लिखना शुरू किया। अब जेलर, जिन्हें ज्योतिष का क ख ग, भी मालूम नहीं था, उन्हें लगा हेमांगद की मानसिक स्थिति ख़राब हो गई है। उन्होंने यह बात जाकर अकबर को बताई। अकबर ने हेमांगद को अपने सामने पेश होने का आदेश दिया।
हेमांगद से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने अकबर को बताया कि वह और कुछ नहीं, कैलेण्डर तैयार कर रहे थे। अगले हजार साल का। अकबर ने सबूत मांगा तो हेमांगद ने उसी समय आने वाले चंद्रग्रहण का टाइम बताया जो एकदम ठीक निकला। बस फिर क्या था। अकबर एक बार फिर खुश। उन्होंने हेमांगद को रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही राजस्व का बकाया भी माफ कर दिया। यहां नोट कीजिए हम कहानी आपको राजपरिवार की सुना रहे हैं लेकिन मुग़लों के वक्त में ये एक जमींदारी खानदान था।
यह भी पढ़ें- दुकानदारों के गाल चीरने वाले अलाउद्दीन खिलजी के आखिरी दिनों की कहानी
साल 1663 में दरभंगा के चौधरी, पुरुषोत्तम ठाकुर की हत्या हुई। तब उनकी पत्नी ने शाहजहां के पास जाकर न्याय मांगा और अपने पति के हत्यारे को फांसी की सजा दिलाई। कुल मिलाकर सरकार तिरहुत के कानून आदि मसलों पर ही मुग़ल ही दखल रखते थे। अब सवाल ये कि अगर ये परिवार जमींदार था। तो इन्हें महाराजा क्यों कहा जाता है?
दरअसल, मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के समय में एक घटना घटी। इस समय सरकार तिरहुत को महिनाथ ठाकुर संभाल रहे थे। जैसा पहले बताया कि यह इलाका मिथिला का हिस्सा था और मिथिला पर दावा करने वालों में एक नेपाल के जमींदार भी थे। हुआ यह कि नेपाल की तरफ वाले मिथिला क्षेत्र ने मुग़ल सल्तनत से बगावत शुरू कर दी। वह टैक्स चुकाने में आनाकानी करने लगे। इस बगावत को रोकने के लिए औरंगज़ेब ने अपनी फौज भेजी। तब महिनाथ ठाकुर ने इस लड़ाई में मुगलों का साथ दिया। नतीजतन मुग़ल बगावत रोकने में सफल रहे।
इस अभियान में महिनाथ की मदद से औरंगज़ेब इतने खुश हुए कि साल 1684 में उन्होंने एक फरमान निकाला। जिसके तहत महिनाथ ठाकुर को बाकी जमींदारों से अलग एक खास ओहदा दिया गया। मुग़ल दरबार की तरफ से उन्हें खिलअत (शाही पोशाक) और माही मरातिब भेंट किए गए। माही मरातिब मुग़लों के समय में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान हुआ करता था। फारसी में माही का मतलब मछली होता है। इस सम्मान में मछली के आकर का एक प्रतीक और झंडा भेंट किया जाता था। महिनाथ ठाकुर को इस सम्मान के साथ तिरहुत सरकार का पूरा इलाका सौंप दिया। साथ ही बंगाल और बिहार के 110 परगने भी उनके अधीन कर दिए गए। यानी महिनाथ ठाकुर का पद राजस्व अधिकारी से बढ़कर क्षेत्रीय शासक का हो गया। यहां से असल में राज दरभंगा की कहानी शुरू होती है।
यह भी पढ़ें- यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार रूस को क्यों सौंप दिए थे? वजह जानिए
जमींदार से राजा तक का सफर
इतिहासकार स्टीफन हेनिंगम अपनी किताब, 'अ ग्रेट एस्टेट ऐंड इट्स लैंडलॉर्ड्स इन कोलोनियल इंडिया' बताते हैं, '18वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में राजपरिवार में एक बड़ा बदलाव हुआ। परिवार के वंशज अब खुद को "ठाकुर" के बजाय "सिंह" कहने लगे। इस परिवतर्न का मकसद साफ था। राज परिवार अब खुद की सामंत दिखाना चाहता था। साल 1720 में उन्हें राजा की उपाधि भी मिल गई। मुग़ल अब कमजोर हो चले थे। क्षेत्रीय ताकतें उभर रही थी। ऐसे में सरकार तिरहुत ने भी अपने कद में इजाफा करना शुरू किया। केवल पैसे से ही नहीं, सैन्य बल से भी।'
साल 1740 की बात है। बंगाल के नवाब अलवर्दी खान ने तिरहुत के राजा पर लगाम लगाने की कोशिश की। तीन बार हमला किया। एक बार तो राजा रघु सिंह के रिश्तेदारों को कैद कर उनकी जमीन भी कब्ज़ा ली। दो मौकों पर रघु सिंह ने समझौता किया लेकिन जब तीसरा मौका आया। उनके उत्तराधिकारी ने युद्ध करने की ठान ली।
यह भी पढ़ें- क्या सच में राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया था?
साल 1750, रघु सिंह के उत्तराधिकारी नरेंद्र सिंह ने अलवर्दी खान को टैक्स चुकाने से साफ़ मना कर दिया। अलवर्दी खान की फौज ने इस बार भी हमले की कोशिश की लेकिन उन्हें हराकर भगा दिया गया। दरभंगा की इस लड़ाई को कंदर्पी घाट की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में जीत ने महाराजा नरेंद्र सिंह की हैसियत में और इजाफा किया और वह एक एक शक्तिशाली सामंत के रूप में स्थापित हो गए।
कहानी में अगला मोड़ आया, 1764 में। नोट कीजिए ये कहानी दरभंगा राज की है लेकिन अब तक हम सरकार तिरहुत कहकर बुला रहे हैं। दरभंगा राज- यह नाम अस्तित्व में आया 1760 के दशक में। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल और बिहार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने कंट्रोल जमा लिया। लिहाजा सरकार तिरहुत के राजा प्रताप सिंह, जिनका मुख्यालय अभी तक मधुबनी के पास भौरा में था। वह अपनी राजधानी दरभंगा ले गए। यहां उन्होंने एक किला बनवाया, जिसके बाद इस रियासत को राज दरभंगा कहा जाने लगा।
कंपनी के साथ कैसे सुधरे रिश्ते?
हालांकि, अंग्रेज़ों ने दरभंगा को कभी प्रिंसली स्टेट का दर्ज़ा नहीं दिया। 1770 से 1800 तक दरभंगा और ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच टैक्स चुकाने को लेकर तनातनी बनी रही। इस स्थिति में बदलाव आया साल 1801 में। दरभंगा के महाराज छत्र सिंह ने कम्पनी के साथ रिश्ते सुधारे। 1813 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी और नेपाल के बीच युद्ध हुआ। इसमें भी छत्र सिंह ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। नतीजा हुआ कि युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की तरफ से छत्र सिंह को महाराजा की उपाधि मिली। छत्र सिंह के बाद उनके बेटे रुद्र सिंह और उनके बाद महेश्वर सिंह और कम्पनी के बीच छोटे मोटे तनावों के बावजूद अच्छा रिश्ता रहा।
यह भी पढ़ें- गंगवाना की लड़ाई: जब 1000 घुड़सवारों ने 40 हजार की सेना को हराया
साल 1857 की क्रांति का एक किस्सा है। क्रांति के दिनों में ब्रिटिश अधिकारियों ने देखा कि महाराजा ने अपने महल के चारों ओर गहरी खाइयां खुदवा दी थीं। जब पूछा गया, तो महाराजा ने दावा किया कि ये खुदाई केवल "सजावटी तालाबों" के लिए थीं। हालांकि, अंग्रेज़ों को शक था कि खूंटा गाड़ने का प्रयास था ताकि लड़ाई की स्थिति में ब्रिटिश फौज अंदर न जा सके। इस शक को बल मिलने का एक और कारण था। 1857 से पहले 1855 में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक और विद्रोह हुआ। आज के झारखंड के जनजातीय इलाकों से उभरा ये विद्रोह, संथाल हूल के नाम से जाना जाता है। चूंकि ये लड़ाई जंगल के इलाकों में लड़ी जानी थी। इसलिए अंग्रेज़ों को हाथियों की दरकार थी। ये हाथी प्रोवाइड कराए थे दरभंगा ने। लेकिन जब 1857 की क्रांति शुरू हुई। दरभंगा की तरफ से अंग्रेज़ों को ऐसी कोई मदद नहीं मिली। दरभंगा के महाराज इंतज़ार कर रहे थे, ऊंट किस करवट बैठेगा।
जीत अंग्रेज़ों की हुई और 1860 में महराजा महेश्वर सिंह की भी मृत्यु हो गई। महेश्वर सिंह के बेटे लक्ष्मेश्वर सिंह नाबालिग थे इसलिए ब्रिटिश प्रशासन ने दरभंगा राज को "कोर्ट ऑफ वार्ड्स" के अधीन कर दिया। कोर्ट ऑफ वार्डस एक ऐसा सिस्टम था। जहां उत्तराधिकारी के नाबालिग होने की स्थिति में शासन ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ चला जाता था। ब्रिटिशर्स के हाथों में ताकत आने के बाद क्या हुआ होगा। आप गेस कर सकते हैं। 1860 में दरभंगा राज की माली हालत ठीक नहीं थी। उन पर 70 लाख रूपये का क़र्ज़ था। कहते हैं तब महाराजा की हालत इतनी दयनीय थी कि उन्हें एक किसान से 300 रूपये उधार लेने पड़े थे। अंग्रेज़ों ने इस मौके को भुनाते हुए, रेवेन्यू कलेक्शन का पूरा सिस्टम ही बदल डाला। और किसानों का खून चूसना शुरू कर दिया।
अंग्रेजी सिस्टम
दरभंगा की कमान अंग्रेज़ों ने मिस्टर फोरलोंग नाम के एक शख्स के हाथ सौंपी। एक अंग्रेज अधिकारी ने फोरलोंग का डिस्क्रिप्शन कुछ यूं दिया है, 'फोरलोंग को दिखावा पसंद था। वह अपने कंधे पर एक लम्बा चोगा डाले रहता था और चार घोड़ों से खींची जाने वाली बग्घी में घूमा करता था। उसके बीच तलवार और कारबाइन से लैस बॉडीगार्ड्स चलते थे।' फोरलोंग को जिम्मा सौंपने के पीछे अंग्रेज़ों का एक खास मकसद था। फोरलोंग दरअसल, नील का व्यापारी था। उसने ठेकेदारी पर नील की खेती करवाई। जिसका 20% कमीशन सीधे अंग्रेज़ों को जाता था। इससे दरभंगा राज का खजाना तो भरा लेकिन आम किसानों पर असर ये हुआ कि 1873-74 में बिहार में जो अकाल पड़ा, दरभंगा उसका मुख्य केंद्र था। लोग दाने दाने को महरूम हो गए। लोगों ने अपनी खेती छोड़ दी।
सिस्टम इतना ख़राब था कि जो जमीन पट्टे पर दी जाती थी, उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता था। भारत में आजादी के बाद जमींदारी प्रथा ख़त्म करने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री नेहरू को इसके लिए लोहे के चने चबाने पड़े थे लेकिन फिर भी सरकार जमींदारी ख़त्म करने को लेकर डटी थी। जमींदारी प्रथा में ऐसा क्या ख़राब था? इसे आप दरभंगा के उदाहरण से समझ सकते हैं। Stephen Henningham अपनी किताब में बताते हैं कि जमीन पट्टे पर दी जाती थी लेकिन कोई लिखित हिसाब नहीं होता था। साल की शुरुआत में किसान को ये तक मालूम नहीं होता था कि साल के अंत में उसे कितना टैक्स चुकाना होगा। अंत में जो पैसा किसान चुकाता, वह मूल का है, या ब्याज- इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं था। सब कुछ पटवारियों के भरोसे चल रहा था और किसान इस सिस्टम में बस पिस रहे थे।
यह किसानों की बात है लेकिन इतिहास किसानों का नहीं राजाओं का होता है। सो वापस दरभंगा राजघराने पर लौटते हैं। साल 1879 में दरभंगा के सिंहासन पर महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह बैठे। अपने पूर्वजों से वह इस मामले में अलग थे कि उनकी पढाई विलायती तौर तरीकों से हुई थी। वे पोलो, बिलियर्ड्स, टेनिस खेला करते थे। और शिकार के लिए इंगलैंड से लाए शिकारी कुत्तों को अपने साथ ले जाते थे। लक्ष्मेश्वर सिंह अपने समय के हिसाब से प्रोग्रेसिव माने जाते थे।
साल 1885- यह साल था जब कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित हुआ। जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए कि यह सत्र बॉम्बे में आयोजित हुआ था लेकिन पहले इसे दरभंगा में कराने की योजना थी। महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने अपना समर्थन भी दिया लेकिन फिर अंग्रेज़ों के प्रेशर के चलते इसे बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया।
कांग्रेस को 10 हजार का दान
1893 में लक्ष्मेश्वर सिंह ने कांग्रेस को दस हजार रूपये का डोनेशन दिया। तब AO ह्यूम- कांग्रेस के फाउंडर ने लक्ष्मेश्वर सिंह को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें वह लिखते हैं कि महाराजा ने दान न दिया होता तो कांग्रेस वहीं ख़त्म हो जाती। ब्रिटिश सरकार के दबाव में लक्ष्मेश्वर सिंह खुद कभी कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल नहीं हुए लेकिन गाहे-बगाहे सीक्रेट तरीके से दान देते रहते थे। इतना ही नहीं उन्होंने साउथ अफ्रीका में गांधी के आंदोलन को भी समर्थन दिया था। गांधी ने इस बाबत उन्हें खत भी लिखा था। गांधी और उनका यह सहयोग आगे बढ़े इससे पहले ही 1898 में लक्ष्मेश्वर सिंह की असामयिक मौत हो गई। लक्ष्मेश्वर सिंह को दरभंगा में सामजिक कार्यों के लिए जाना जाता है। अंग्रेज़ी शिक्षा से लेकर विधवा पुनर्विवाह- जैसा पहले बताया, लक्ष्मेश्वर सिंह ने तमाम प्रोग्रेसिव विचारों को समर्थन दिया। हालांकि उनकी मौत के बाद कहानी पलट गई।
लक्ष्मेश्वर सिंह की मौत के बाद गद्दी पर बैठे उनके छोटे भाई रामेश्वर सिंह और वह अपने भाई के बिल्कुल उलट थे। पूरी तरह से धार्मिक और परंपरावादी। साल 1900 की एक घटना है। दिल्ली में हिंदूवादी संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। नजारा देखने लायक था, एक लाख लोगों के एक जुलूस। जिसका नेतृत्व कर रहे थे - रामेश्वर सिंह! महाराजा नंगे पैर थे और हाथों मे थी वेदों की प्रति। मजेदार बात यह कि यही महाराजा जो नंगे पांव जुलूस निकालते थे, घर पर विदेशी जूते पहनते थे! इतना ही नहीं अंग्रेजी शराब का बड़ा शौक था। हालांकि, बस अपने करीबी दोस्तों के साथ ही पीते थे। घर पर रवैया कड़क था। जब घुड़सवारी पर निकलते, रास्ते में मिले तो झुककर प्रणाम करना जरूरी। वरना? कोड़े पड़ते!
महाराजा के नाम से साथ कुछ उपलब्धियां भी जुड़ी, मसलन 1911 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो इसके लिए दान देने वालों में रामेश्वर सिंह भी थे। दरभंगा की दो यूनिवर्सिटी आज भी दरभंगा के पुराने महल में चलती हैं। रामेश्वर सिंह दरभंगा के सेकेण्ड लास्ट महाराजा रहे, उनके बाद आगे कामेश्वर सिंह। जिन्हें आधुनिक दरभंगा का निर्माता माना जाता है।
आख़िरी महाराजा
जुलाई 1929 में बाईस वर्ष की आयु में कामेश्वर सिंह ने दरभंगा के महाराजाधिराज के रूप में पदभार संभाला। धार्मिक मामलों में वेह अपने पिता के विपरीत, अपने चाचा लक्ष्मेश्वर सिंह की तरह थे - कुछ उदार। उदाहरण- उन दिनों समंदर पार करना धर्म के खिलाफ माना जाता था। इसके बावजूद महाराजा अक्टूबर 1930 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। वह सम्मेलन जिसका गांधी और कांग्रेस ने बहिष्कार किया था।
दिलचस्प बात यह कि इस मामले में उन्होंने गांधी की मंशा को नजरअंदाज किया था लेकिन गांधी की पहली मूर्ति बनवाने वाले भी महाराज कामेश्वर ही थे। अब यहां एक और कमाल की बात। गांधी की पहली मूर्ति का मूर्तिकार और कोई नहीं, विंस्टन चर्चिल का चचेरा भाई था। वही चर्चिल जो गांधी के बारे में कहते थे, क्यों वह बुड्ढा मरा नहीं अब तक।
कामेश्वर सिंह की एक और रोचक बात थी -गाड़ियों के प्रति प्रेम! उनके पास दर्जनों लक्जरी कारें थीं और एक खास रेलवे कोच भी, जिसे वह ट्रेन यात्रा के दौरान इस्तेमाल करते थे। 1940 में अपनी वरिष्ठ पत्नी की मृत्यु के बाद, उन्होंने उनकी व्यक्तिगत उपयोग के लिए आरक्षित रोल्स रॉयस को दरभंगा अनाथालय को दान कर दिया।
दरभंगा महल का एक अनूठा पहलू था - महाराजा का "फूड टेस्टर"! हर भोजन से पहले खाना चखकर देखने वाला। आमतौर पर ज़हर के डर से राजा-महाराजा ऐसा किया करते थे लेकिन महाराज कामेश्वर के केस में ज़हर से ज्यादा बुरे स्वाद का डर था। इसीलिए उनकी रसोई में 12 रसोइये थे, जिनमें से 2 सिर्फ मिठाइयां बनाने का काम करते थे।
महाराज को विदेशी चीजों का भी बड़ा शौक था, खासकर स्कॉच का! उनके पास स्कॉच और विदेशी शराबों का एक बड़ा संग्रह था। किस्सा है कि एक बार नेहरू ने उन्हें कांग्रेस में शामिल होने का आग्रह किया। कामेश्वर सिंह का जवाब? "नहीं!" क्यों? क्योंकि कांग्रेस का शराब से परहेज़ का संकल्प उनके स्कॉच के प्रति प्रेम से मेल नहीं खाता था!
रोचक किस्सों से इतर कामेश्वर सिंह कई और उपलब्धियों के लिए भी जाने जाते हैं। पटना विश्विद्यालय, मिथिला पोस्टग्रेजुएट रिसर्च इंस्टिट्यूट, दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी - इन तमाम संस्थानों के निर्माण में महाराजा कामेश्वर सिंह ने योगदान दिया था। आजादी के बाद राज्य सभा के मेंबर चुने गए। इस दौरान नेहरू से भिड़ने से भी नहीं चूके। जमीदारी उन्मूलन क़ानून के विरोध में कामेश्वर सिंह ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। एक बार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था - "आप हमारी जमीन बेशक ले लें, पर इतिहास नहीं बदल सकते। हमारे पूर्वजों ने इस देश की सेवा इसलिए नहीं की थी कि आप एक झटके में सब कुछ छीन लें।"
दरभंगा के महाराज ने एविएशन के फील्ड में भी खास योगदान दिया था। 1950 में महाराज ने एक एयरलाइंस की शुरुआत भी की। दरभंगा एयरलाइंस। हवाई उड़ान से जुडी एक और उपलब्धि में महाराज कामेश्वर सिंह ने योगदान दिया था। 3 अप्रैल 1933 की तारीख। पूर्णिया के लाल बालू मैदान से एक खास उड़ान शुरू हुई। यह एवेरेस्ट के ऊपर उड़ने वाली पहली फ्लाइट थी। इस काम में दरभंगा के महाराज का खास रोल था। वित्तीय सहायता के अलावा महाराजा ने पूरी टीम को पूर्णिया में अपने दरभंगा हाउस में ठहराया। खुद भी वहीं कैंप किया ताकि मिशन सफल हो।
हमने आपको अभी बताया था कि महाराज ने एक खास रेल सलून बनाया था। अब सलून बनाया था, तो पटरियां भी होंगी। अपने वक्त दूसरे अमीर घरानों की ही तरह राज दरभंगा ने भी अपने इलाके में रेल नेटवर्क बनवाया। इसे कहा गया तिरहुत रेलवे। आज़ादी के बाद यह भारतीय रेल का हिस्सा बना। महाराजा ने तीन स्टेशन भी बनवाए थे। एक उनके घर के लिए एक जो आम पब्लिक के लिए था और तीसरा खास मेहमानों के लिए। इन तमाम बातों के अलावा दरभंगा राजघराने को जाना जाता है, स्पोर्ट्स और म्यूजिक में उनके योगदान के लिए। राज दरभंगा के राजा संगीत, कला और संस्कृति के बहुत बड़े समर्थक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, गौहर जान, पंडित राम चतुर मल्लिक, इंडियन क्लास्सिकल म्यूजिक के ये दिग्गज दरभंगा राज से जुड़े थे। आज भी दरभंगा द्रुपद के लिए जाना जाता है। बाकायदा ध्रुपद की तीन बड़ी शैलियों में से एक का नाम "दरभंगा घराना" है।
दरभंगा के खजाने का क्या हुआ?
आजादी के वक्त दरभंगा के महाराज की सालाना आमदनी थी-पूरे 55 लाख रुपये! उस वक्त के हिसाब से यह बहुत पैसा था। लिहाजा दरभंगा के राजा दूसरे छोटे-मोटे राजघरानों के बैंकर बन गए थे। डुमराव, टेकारी, कूच बिहार के राजा - सभी जब कंगाली में आते, तो दरभंगा से कर्ज लेते। कभी-कभी अपने खानदानी गहने भी बेच देते थे। बस यहीं से शुरू हुआ दरभंगा का वह अनमोल रत्न भंडार, जो हैदराबाद के निज़ाम के खज़ाने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था।
क्या-क्या मौजूद था इस खजाने में?
दरभंगा के गहनों में सबसे मशहूर था मराठा पेशवाओं का नौलखा हार। मोतियों, हीरों और पन्नों का ये लंबा हार दुनिया के सबसे शानदार हारों में गिना जाता था। मूल रूप से यह पेशवा बाजीराव प्रथम का था, जिन्होंने इसे 9 लाख रुपये में बनवाया था - इसीलिए नाम पड़ा 'नौलखा'। उनके बाद, हर पीढ़ी के पेशवाओं ने इसमें और रत्न जुड़वाए। 1900 के दशक तक इसकी कीमत बढ़कर 90 लाख रुपये हो गई थी! 1857 की क्रांति के बाद, हारे हुए नानासाहब पेशवा इसे अपने साथ नेपाल ले गए। वहां इसे औने-पौने दामों में नेपाल के प्रधानमंत्री राणा जंग बहादुर को बेच दिया। राणा ने इसके सारे बड़े पन्ने और माणिक निकाल लिए। बाद में राणा के उत्तराधिकारी ने इसे दरभंगा के राजा को बेच दिया - वही एकमात्र शख्स थे जो उस वक्त इसे खरीद सकते थे।
1901 में दरभंगा ने नेपाल के राणाओं से दो और मशहूर चीजें खरीदीं - नानासाहब की 'शिरोमणि' मुहर, जिसमें तीन इंच लंबा एक अकेला पन्ना जड़ा था और 'पेशवा हीरा' - एक बड़ा सफेद हीरा, जिसे दरभंगा के महाराजा अंगूठी की तरह पहनते थे।
दरभंगा के संग्रह में एक और खास चीज थी - फ्रांस की आखिरी रानी मेरी एंटोइनेट का हार! यह वही हार था जो 1770 में उनकी शादी पर पेरिस शहर ने उन्हें तोहफे में दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग परिवार के पास चला गया।
1930 के दशक में एक ऑस्ट्रियाई राजकुमारी ने इसे नीलामी में रखा। महाराजा कामेश्वर सिंह, जो ऐतिहासिक गहनों के शौकीन थे, ने सफल बोली लगाई और कुछ लाख रुपये देकर इसे अपने संग्रह में शामिल कर लिया। दरभंगा के महाराजा ने रूस के ज़ार के कई जवाहरात भी खरीदे थे।
इनके अलावा दरभंगा के संग्रह में दुनिया का सबसे बड़ा नक्काशीदार पन्ना भी था - 'ग्रेट मुग़ल एमरल्ड'। 217 कैरेट का यह पन्ना करीब 2 इंच लंबा, 1.75 इंच चौड़ा और आधा इंच मोटा था। माना जाता है कि यह मुग़ल बादशाहों का था, जिस पर कुरान की आयतें नक्काशी की गई थीं। कूच बिहार के महाराजा ने इसे कर्ज के बदले गिरवी रखा था और जब वह कर्ज नहीं चुका पाए तो यह दरभंगा के पास आ गया। दरभंगा के खजाने का एक संबंध भारत के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन से भी था। रमन रत्नों के शौक के लिए जाने जाते थे। अपनी प्रयोगशाला में अक्सर वह हीरों का अध्ययन करते थे। एक बार शोध के लिए उन्हें एक बड़े हीरे की जरूरत पड़ी और दरभंगा के महाराजा ने उन्हें दो दिन के लिए 140 कैरेट का हीरा उधार दे दिया! ये वही 'पेशवा हीरा' था, जिसे महाराजा अंगूठी की तरह पहनते थे।
दरभंगा के संग्रह में और भी कई अनोखी चीजें थीं:
- अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह का एक प्याला, जो एक ही पन्ने से बना था
- धौलपुर के राणा का मोतियों का मुकुट
- मुर्शिदाबाद के नवाबों के गहने
इन सभी गहनों को महाराजाओं के दफ्तर में रखा गया था लेकिन अब ये कहां हैं? किसी को नहीं मालूम।
मार्च 2024 में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी रिपोर्ट के अनुसार, महाराजा कामेश्वर सिंह के पास हजारों एकड़ जमीन, इमारतें, कंपनियां, अरबों के जेवरात, यह सब कुछ था लेकिन महाराजा ने अपनी संपत्ति का वारिस एक ट्रस्ट को बनाया। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी तीन लोगों के पास थी। एक महाराज के बहनोई- दो बाहर के लोग। खुद अपनी रानियों के लिए महाराज महज पांच हजार महीना रकम तय कर गए जबकि महाराजा की कुल संपत्ति आज के हिसाब से आकलन किया जाए तो चार लाख करोड़ के बराबर थी। जमीन से लेकर शेयर तक। सब शामिल था। केवल जवाहरातों की ही कीमत 200 करोड़ के आसपास थी लेकिन मिलकर सब लूटखसोट लिया गया।
कामेश्वर सिंह की बड़ी पत्नी राजलक्ष्मी की डायरी में एक जिक्र आता है। मार्च 1967 में वह लिखती हैं, 'ज्वेलर आए। ट्रस्ट वालों ने सारा गहना उसे बेच दिया गया। मुझसे एक बार भी नहीं पूछा।' मार्च 1967 में इस तथाकथित नीलामी में करोड़ों के जवाहरात बॉम्बे के मशहूर जौहरी नानूभाई झवेरी को बेच दिए गए। कितनी कीमत पर - मात्र 70-75 लाख। जबकि एक यूरोपियन फर्म ने इनकी कीमत 2 करोड़ पाउंड आंकी थी। लूट का यह सिलसिला- 1967 से नहीं 1962 से ही शुरू हो चुका था। महाराजा की मौत के तुरंत बाद। नवम्बर 1962- ट्रस्टियों ने महाराजा के दो हवाई जहाज भारत सरकार को दान में दे दिए। इसके बाद तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को दरभंगा बुलाया गया। उन्हें सोने से तौला गया और ये सारा सोना भारत सरकार के डिफेन्स फंड में डाल दिया गया। आपको लग सकता है कि सरकार को दान देने में क्या ही दिक्कत?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दरभंगा राज पर लिखी गई किताब 'द क्राइसिस ऑफ सक्सेशन' के लेखक तेजकर झा का कहना दर्ज़ है। तेजकर झा कहते हैं, 'ट्रस्ट के एग्जीक्यूटर पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे लक्ष्मीकांत झा थे। वह लॉ कमिशन का अध्यक्ष बनना चाहते थे और मोरारजी देसाई को तोले जाने का आयोजन इसी कवायद का नतीजा था।'
ऐसा ही कुछ हाल महाराजा की कोठियों का भी हुआ। इलाहाबाद-कलकत्ता-सौराष्ट्र- तमाम जगहों की कोठियां बेच दी गई। बाकायदा इलाहबाद की कोठियां तो ट्रस्टी मुकुंद झा, जो महाराजा के बहनोई थे, ने अपने बेटे के नाम करवा लीं। इसके बाद नंबर आया महाराज की फैक्ट्रियों का। अपने जमान में एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल - अशोक पेपर मिल। लोहट की चीनी मिलें। एक-एक करके सब अधिग्रहीत हुई और एक दशक के भीतर बंद भी हो गईं। इमरजेंसी के दौरान सरकारी अधिग्रहण के नाम पर दरभंगा राज का मुख्य कार्यालय ले लिया गया। यह सब हुआ बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के इशारे पर। 300 बीघा जमीन के लिए मात्र 70,000 रुपये मुआवजा दिया गया।
ट्रस्ट में महाराजा के शेयर भी थे। इन्हें भी औने-पौने दामों पर बेच दिया गया। कुल मिलाकर कहा जाए तो दरभंगा राज की निशानियों के नाम पर आज बस कुछ पुरानी इमारतें बची हैं। जिन्हें देखकर शायद ही कोई कह सके कि एक समय में दरभंगा के महाराज भारत के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हुआ करते थे। बहरहाल, इसी नोट पर आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं।