इस्लाम के बारे में भीमराव आंबेडकर के विचार क्या थे? विस्तार से समझिए
डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती आज है। संविधान निर्माता के नाम से मशहूर हुए डॉ. आंबेडकर अपने विचारों के लिए आज भी जाने जाते हैं। आइए तमाम धर्मों के बारे में उनके विचार जानते हैं।
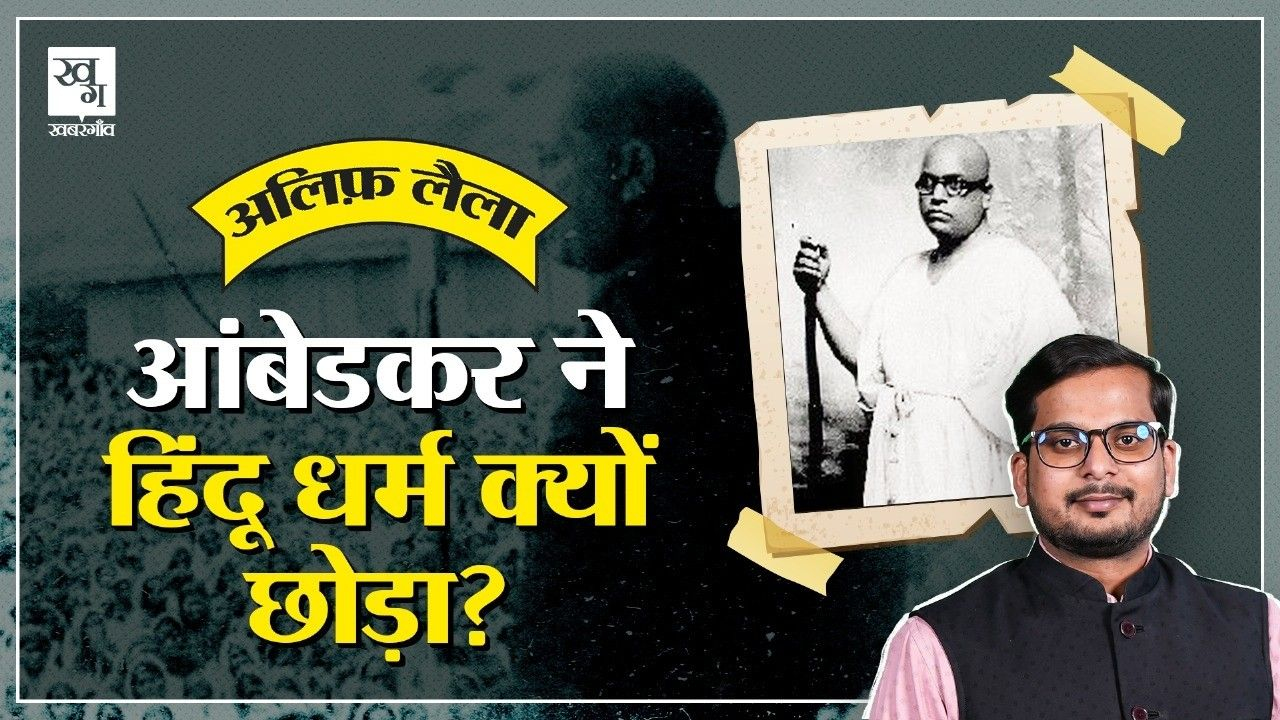
डॉ. भीमराव आंबेडकर की कहानी, Photo Credit: Khabargaon
साल 1901 की बात है। तब डॉ. आंबेडकर का परिवार सतारा में रहता था। उनकी मां का देहांत हो चुका था। उनके पिता फौज से रिटायर होकर कोरेगांव में खजांची का काम करते थे। एक बार गर्मी की छुट्टियों में पिता ने आंबेडकर और उनके भाई-बहनों को कोरेगांव बुलाया। वे सब रेलवे स्टेशन गए। वहां से ट्रेन मसूर स्टेशन तक गई। यह कोरेगांव का सबसे पास वाला स्टेशन था। पिता जी ने कहा था कि वह स्टेशन पर अपना चपरासी भेजेंगे लेकिन आंबेडकर और उनके भाई-बहन स्टेशन पर इंतज़ार करते रहे। एक घंटे तक कोई नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने बच्चों को देखा और पूछा, 'सब चले गए, तुम लोग यहाँ क्यों हो?'
आंबेडकर ने बताया कि उन्हें कोरेगांव जाना है। वे अपने पिता या उनके चपरासी का इंतज़ार कर रहे हैं। डॉ. आंबेडकर ने लिखा है, 'हमने अच्छे कपड़े पहने थे। हमारी बोली से कोई नहीं जान सकता था कि हम अछूत बच्चे हैं।' इसलिए स्टेशन मास्टर को लगा कि वे ब्राह्मण बच्चे हैं। वह उनकी परेशानी देखकर दुखी हुए। थोड़ी देर बाद स्टेशन मास्टर ने पूछा, 'तुम कौन हो?' आंबेडकर ने जवाब दिया, 'हम महार हैं।' यह सुनते ही स्टेशन मास्टर का व्यवहार बदल गया। वह वापस अपने कमरे में चले गए। आंबेडकर और उनके भाई-बहन परेशान हो गए। स्टेशन के पास कुछ बैलगाड़ी वाले थे पर कोई भी उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं था क्योंकि वे अछूत थे। वे गाड़ी वाले दोगुना किराया देने को भी तैयार थे, फिर भी कोई राजी नहीं हुआ।
मुसलमान बताकर मांगा पानी
फिर स्टेशन मास्टर ने एक तरीका निकाला। उन्होंने आंबेडकर से पूछा, 'क्या तुम बैलगाड़ी चला सकते हो?' आंबेडकर ने 'हां' कहा। स्टेशन मास्टर ने एक गाड़ी वाले से बात की। वह दोगुना किराया लेगा लेकिन गाड़ी नहीं चलाएगा। वह बस गाड़ी के साथ चलेगा। आंबेडकर और उनके भाई-बहन गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चलने लगी। चलते-चलते रात हो गई। उनके पास घर से आया खाना तो था लेकिन पीने का पानी खत्म हो गया था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक चुंगी वाले की झोपड़ी दिखी। आंबेडकर ने सोचा कि उससे पानी मांगा जाए। तभी बैलगाड़ी वाले ने कहा, 'वह हिन्दू है। वह महारों को पानी नहीं देगा। तुम कहना कि तुम मुसलमान हो। शायद पानी मिल जाए।'
यह भी पढ़ें- सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के 'कसाइयों' की कहानी
आंबेडकर ने चुंगी वाले से पानी मांगा। चुंगी वाले ने पूछा, 'कौन हो?' आंबेडकर ने कहा, 'हम मुसलमान हैं।' आंबेडकर अच्छी उर्दू बोल लेते थे पर फिर भी बात नहीं बनी। चुंगी वाले ने कहा, 'यहां पानी नहीं है। दूर पहाड़ी पर है। वहां से ले आओ।' तब तक बहुत रात हो चुकी थी। पहाड़ी पर जाना मुमकिन नहीं था। इसलिए सबने बैलगाड़ी में ही बिस्तर लगाया और वहीं सो गए। आंबेडकर ने लिखा, 'मैं सोच रहा था, हमारे पास खाना तो था। हमें भूख भी लगी थी पर पानी नहीं मिला। हमें पानी के बिना भूखे सोना पड़ा और पानी इसलिए नहीं मिला, क्योंकि हम अछूत थे।'
इस घटना के वक्त डॉक्टर आंबेडकर की उम्र मात्र 9 साल की थी। वह लिखते हैं कि इस घटना ने उनके दिमाग में गहरा असर डाला। ऐसा नहीं था कि उन्हें पहली बार छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल में वह बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। उन्हें एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। वह अपने साथ एक बोरा लेकर आते थे जिसे सफाई करने वाला भी नहीं छूता था। पानी पीने के लिए भी एक चपरासी उन्हें घड़े से पानी निकालकर देता था। अगर चपरासी न हो तो उन्हें प्यासा ही रहना पड़ता था। यहां तक कि धोबी भी उनके कपड़े नहीं धोते थे। छुआछूत के चलते नाई भी उनके बाल काटने से इनकार कर देते थे लेकिन इससे पहले आंबेडकर के मन में कभी ये सवाल नहीं उठा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आंबेडकर लिखते हैं, ‘अब तक मुझे लगता था कि छुआछूत एक सामान्य चीज है। कुछ लोग होते हैं, जिन्हें दूसरे लोग छूना नहीं चाहते।’
यह भी पढ़ें- मेवाड़ के राजा राणा सांगा अपनी गद्दी छोड़ना क्यों चाहते थे?
कोरेगांव जाते हुए जो अनुभव हुआ। उसने आंबेडकर को जातिवाद और छुआछूत को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर दिया। धर्म में आमूल-चूल परिवर्तन हुए बिना, जाति व्यवस्था नहीं ख़त्म हो सकती। यह समझते हुए मृत्यु से महज दो महीने पहले अक्टूबर, 1956 में आंबेडकर ने धर्म बदल लिया। नागपुर में लाखों दलितों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म ही क्यों? आंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? हिंदू धर्म छोड़ने के पीछे आंबेडकर ने क्या कारण बताए? इस्लाम ईसाइयत और सिख धर्म के बारे में आंबेडकर का क्या विश्लेषण था? आज आंबेडकर जयंती के मौके पर इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे।
धर्मों पर आंबेडकर के विचार क्या थे?
आंबेडकर किस धर्म के बारे में क्या सोचते थे। एक लाइन में पाले तैयार कर लेना आसान है लेकिन आदमी पेचीदा शय होता है। आप अपने ही अंदर आर्गुमेंट और काउंटर आर्गुमेंट की लड़ाई लड़ते हैं और यह सब एक दिन में नहीं होता। कोई भी बड़ा निर्णय सालों की जद्दोजहद के बाद नतीजे में आता है। आंबेडकर के धर्म परिवर्तन की दिशा समझने के लिए हमें 1923 के आसपास के समय में चलना होगा। आंबेडकर लंदन से पढाई करके वापस लौटे हैं। लगभग एक दशक से ज्यादा समय विदेश में बिताया, इस दौरान उन्होंने खुद लिखा है कि विदेश में छुआछूत भूल चुके थे लेकिन जब बड़ौदा आए, दोबारा वही हुआ जो बचपन से उन्होंने झेला था।
बड़ौदा में उन्हें रहने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। हिंदू होटलों में कोई उन्हें रखने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपने एक ईसाई दोस्त से पूछा लेकिन उस दोस्त ने भी मदद नहीं की। आखिर में, वह एक पारसी सराय (धर्मशाला) में गए। सराय के मालिक ने भी मना कर दिया। उसने कहा कि यहां सिर्फ पारसी ही रह सकते हैं। बहुत मुश्किल से वह माना। उसने डॉ. आंबेडकर को सबसे ऊपर एक कमरा दिया। कमरा बहुत अंधेरा था, वहां लाइट भी नहीं थी। आसपास कोई बात करने वाला नहीं था। आंबेडकर बताते हैं कि उन्हें बहुत अकेला लगता था। उन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही सरकारी घर मिलेगा। आंबेडकर कुछ दिन उसी सराय में रहे। फिर एक दिन 10-12 पारसी आए। उन्होंने आंबेडकर को कमरे से निकाल दिया। आंबेडकर ने लिखा, 'उस दिन मुझे समझ आया। जो इंसान हिंदुओं के लिए अछूत है, वह पारसियों के लिए भी अछूत है।'
यह भी पढ़ें- भारत में मचा हंगामा, पाकिस्तान में कैसे काम करता है वक्फ? समझिए
ऐसी तमाम घटनाओं के चलते आंबेडकर जाति व्यवस्था के सवाल पर गहराई से अध्ययन करने लगे। पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, जवाब किताबों में ढूंढा, विश्लेषण किया। क्यों होती है जाति? अछूत क्यों माना जाता है? भेदभाव क्यों होता है? इन तमाम सवालों का पहला जवाब गरीबी था लेकिन आंबेडकर के पिता अच्छी खासी नौकरी करते थे। खुद वह लंदन से पढ़कर आए थे। इसका मतलब गरीबी कारण नहीं हो सकती। गरीब फिर भी अमीर बन सकता है लेकिन एक पिछड़ी जाति का आदमी कितनी मेहनत कर ले , कभी अगड़ी जातियों के बराबर नहीं समझा जाएगा। यह बात आंबेडकर को समझ आ गई थी। इसलिए शुरुआत से ही उन्होंने धर्म की आलोचना शुरू कर दी।
हिंदू धर्म क्यों छोड़ा?
धर्म के मामले में आंबेडकर की सोच में दो पहलू दिखाई देते हैं। पहला सांसारिक पक्ष- यानी पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा। दूसरा आध्यात्मिक पक्ष- यानी निजी जीवन में धर्म का महत्व। पहले सांसारिक पक्ष की बात करते हैं। साल 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के तहत मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुस्लिमों की अलग सीटें थीं और उन पर वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते थे। आंबेडकर का मानना था दलितों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए यह रास्ता अपनाना होगा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया।
तब उसके सामने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठी। यानी दलितों के लिए अलग सीट, जिनमें सिर्फ दलित ही वोट करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया। गांधी इनमें प्रमुख थे। इसी समय आंबेडकर अपने अखबार "बहिष्कृत भारत" में हिन्दू धर्म के विरोध में लिखना शुरू किया। यह एक प्रकार का पोलिटिकल प्रेशर था। यानी हिन्दू नहीं सुधरेंगे तो उन्हें राजनैतिक नुकसान होगा। 1929 में ‘बहिष्कृत भारत’ के एडिटोरियल लेख ‘नोटिस टू हिंदूइज़्म’ में आंबेडकर ने साफ़ लिखा, ‘धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो।’
यह भी पढ़ें- Kesari Chapter 2: चेट्टूर शंकरन नायर की पूरी कहानी क्या है?
इस समय तक आंबेडकर का पूरा परियोजन पिछड़ों को अधिकार दिलाने का था। इसी कारण गांधी के बॉयकॉट के बावजूद वह राउंड टेबल कॉन्फेरेन्स में लंदन गए। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग ब्रिटिश सरकार मान भी गई लेकिन फिर गांधी अड़ गए। गांधी का मानना था कि इससे हिन्दू समाज बंट जाएगा। यरवदा जेल में उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी की जिद के आगे आंबेडकर को झुकना पड़ा और अंततः 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ। जिसके चलते सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय पिछड़ों के लिए विधायिका में रिजर्वेशन लागू हो गया। आंबेडकर इसके बाद और मुखर हो गए।
13 अक्टूबर 1935 को येवला हजारों लोगों के सामने आंबेडकर ने घोषणा की, 'मैं हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा।' यहां से आंबेडकर के विचारों में एक लम्बा मंथन शुरू हुआ। जिसकी परिणीति हुई साल 1956 में। जब नागपुर में उन्होंने लाखों पिछड़ों के साथ मिलकर बौद्ध धर्म की शरण ले ली। 1935 से 1956 के बीच आंबेडकर के सैड़कों भाषण, किताबें और लेख हैं, जिनमें उन्होंने अलग-अलग धर्मों को लेकर अपने विचार दिए हैं। इनमें सबसे चर्चित है - ‘मुक्ति कोण पथे’ यानी ‘मुक्ति का मार्ग क्या है।’
साल 1936 में महार सम्मलेन के दौरान आंबेडकर ने यह भाषण दिया था। जिसमें वह सिलसिलेवार तरीके से अपने तर्क रखते हैं। हिन्दू धर्म की आलोचना में आंबेडकर ने पाया कि हिन्दू समाज में जाति का कांसेप्ट धर्म शास्त्रों से आया। इन्हें वह दो भागों में बांटते हैं -
उपनिषद- जो सिद्धांत या दर्शन की बात करते हैं
दूसरे- पुराण और स्मृतियां - जिनमें रोजमर्रा के नियम बताए गए हैं।
आंबेडकर कहते हैं, 'हिन्दू समाज नियमों पर चलता है और चूंकि धर्म सनातन है, तो इन नियमों में बदलाव आना मुश्किल है।' ‘मुक्ति कोण पथे’ में ही आंबेडकर दलितों और सवर्ण जातियों के बीच संघर्ष को क्लास स्ट्रगल का नाम देते हैं। वह कहते हैं, 'यह दो व्यक्तियों या दो समूहों के बीच का संघर्ष नहीं बल्कि दो वर्गों के बीच का संघर्ष है। यह एक आदमी पर दूसरे के प्रभुत्व या अन्याय का सवाल नहीं। बात दो वर्गों की है। दो वर्गों का संघर्ष तब पैदा होता है, जब आप उच्च वर्गों के साथ समानता पर जोर देते हैं।' ऐसे तमाम तर्कों के बल पर आंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि हिन्दू धर्म छोड़े बिना, चीजें बदलने नहीं वाली लेकिन अब अगला बड़ा सवाल। हिन्दू धर्म छोड़े तो जाएं कहां?
यह भी पढ़ें- सुखविंदर कौर के राधे मां बनने और विवादों में आने की कहानी
आंबेडकर जानते थे कि भारतीय समाज में धर्म गहरे में जुड़ा हुआ है। संगठित होने के लिए पिछड़ों को एक धर्म की छतरी के नीचे आना होगा। लेकिन कौन सा धर्म? इस सवाल के जवाब में उन्होंने सिख, ईसाई, बौद्ध तमाम धर्मों का विश्लेषण किया और अपने लिखे में वह बार बार इनके बीच तुलना करते हैं। 1928 के आसपास, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग उठी थी। तब आंबेडकर के लेखों में इस्लाम का चिंतन दिखाई देता है। खासकर इस्लाम का सामाजिक एस्पेक्ट।
आंबेडकर लिखते हैं, 'किसी दलित पर सवर्ण के अत्याचार का मामला उठता है तो इसे धर्म के अंदर की बात कह दिया जाता है लेकिन मुस्लिमों के साथ ऐसा नहीं है। वे संख्या में कम हैं लेकिन एक भी मुस्लिम पर आंच आए, तो वे एकजुट हो जाते हैं।' इसके अलावा मुस्लिमों के पास रिप्रेजेंटेशन था। आंबेडकर को लगा, "दलितों को ताकत की जरूरत है। यह ताकत किसी दूसरे धार्मिक समुदाय में शामिल होकर ही मिल सकती है।' मुस्लिम समुदाय में शामिल होने के लिए आंबेडकर यह तर्क दे रहे थे। हालांकि, जैसा पहले बताया, धर्म उनके लिए सिर्फ सांसारिक पहलू नहीं था। आध्यात्मिक पक्ष पर भी वह इतना ही जोर देते थे और इसी वजह से उन्होंने इस्लाम की भी वैसी ही आलोचना की, जैसी हिंदी धर्म की की थी।
इस्लाम पर आंबेडकर
1940 में आंबेडकर ने 'पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया' नामक पुस्तक लिखी। जिसके अगले दो संस्करण, 1945 और 1946 में छपे। यह किताब मूलतः पाकिस्तान की मांग से संबंधित थी लेकिन इसमें इस्लाम की धर्म के रूप में पर्याप्त आलोचना शामिल थी। आंबेडकर लिखते हैं, 'हिन्दू धर्म लोगों को बांटता है लेकिन इस्लाम एक साथ जोड़ता है - यह बात आधी सच है। इस्लाम लोगों को मुस्लिम और गैर मुस्लिम में बांटता है। इस्लाम का भाईचारा सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। यह भाईचारा सिर्फ मुस्लिमों के लिए है।' राष्ट्रीयता के सवाल पर आंबेडकर लिखते हैं, 'इस्लाम में सामाजिक स्वराज का सिस्टम है लेकिन यह स्थानीय स्वराज के सिस्टम से पूरी तरह असंगत है क्योंकि एक मुसलमान की निष्ठा उस देश में नहीं है जिसमें वह रहता है, बल्कि उनकी पहली निष्ठा धर्म के प्रति है।'
यह भी पढ़ें- युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल फायदेमंद या अपना नुकसान, इतिहास से समझिए
ध्यान दीजिए यह वह दौर है जब अलग पाकिस्तान बनने की मांग जोरों पर थी और कई मुस्लिम नेता जो 1920 तक गांधी के साथ चलते थे। अब अलग देश की मांग कर रहे थे। इस रवैये की आलोचना करते हुए आंबेडकर ने लिखा, 'मुस्लिम कैनन लॉ के अनुसार, दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। दार उल हर्ब और दारु उल इस्लाम। यानी वे देश जहां इस्लाम का शासन है और दूसरे वे, जहां मुस्लिम रहते तो हैं लेकिन इस्लाम का शासन नहीं है।'
आगे वह लिखते हैं, 'इस्लाम एक सच्चे मुसलमान को कभी यह अनुमति नहीं देगा कि वह भारत को अपनी मातृभूमि और हिन्दुओं को अपना भाई माने।' इस तरह एक-एक करके आंबेडकर मुस्लिम कट्टरता के कई पक्षों की आलोचना करते हैं। 1929 तक वह इस्लाम में कन्वर्ट होने की बात कह रहे थे लेकिन बाद में उन्हें अहसास हुआ कि मुस्लिम समाज भी जाति व्यवस्था से अछूता नहीं है।
आंबेडकर लिखते हैं, 'इस्लाम भाईचारे की बात करता है। हर कोई मानता है कि इस्लाम गुलामी और जाति से मुक्त होगा। गुलामी कानूनी रूप से ख़त्म हो चुकी है लेकिन जब यह कायम थी, इस्लामी देशों में इसे समर्थन मिलता रहा।' इस्लाम में व्याप्त जाति व्यवस्था पर आंबेडकर 1901 के बंगाल सेंसस का हवाला देते हैं। जिसके अनुसार मुस्लिम समाज भी जातियों में बंटा हुआ था। सबसे ऊपर आते थे अशरफ- इसके बाद अज़लफ और सबसे नीचे अर्ज़ल। हिंदू समाज की तरह इनमें भी भेदभाव होता था और अक्सर नीची जाति के मुस्लिम अपर कास्ट से शादी नहीं कर सकते थे।
यह भी पढ़ें- 300 साल पहले भी औरंगजेब की कब्र पर हुई थी राजनीति, पढ़िए पूरी कहानी
जाति प्रथा के अलावा आंबेडकर ने इस्लाम में महिलाओं की ख़राब स्थिति के बारे में भी लिखा है, 'पर्दा सिस्टम के चलते महिलाएं अलग-थलग कर दी गई हैं। बुर्का पहने हुई महिलाएं जो सड़कों पर चलती हुई दिखती हैं- यह अलगाव महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। वे आमतौर पर एनीमिया, टीबी और पायरिया की शिकार होती हैं। पर्दा मुस्लिम महिलाओं को मानसिक और नैतिक पोषण से वंचित करता है।' इस्लाम के राजनैतिक पक्ष पर आंबेडकर लिखते हैं, 'मुसलमानों को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी ज्यादा दिलचस्पी धर्म में है। अपने नेता से वे उम्मीद भी ऐसी ही करते हैं कि उनका उम्मीदवार मस्जिद के लिए नया कालीन दे दे या मस्जिद की मरम्मत करवा दे।'
इन तमाम बातों के निष्कर्ष में आंबेडकर ने लिखा, 'हिंदू समाज की कमी निकालते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिम समाज बेहतर है लेकिन उनमें भी वह तमाम बुराइयां मौजूद हैं, जो हिन्दू समाज में व्याप्त हैं। जैसे चाइल्ड मैरिज, पर्दा सिस्टम, जातिवाद। इन निष्कर्षों के बल पर आंबेडकर ने इस्लाम में कन्वर्ट होने का विचार त्याग दिया।' हालांकि, राजनैतिक रूप से कई मोर्चों पर वे और मुस्लिम लीग साथ खड़े दिए। सेपरेट इलेक्टोरेट के मसले पर मुस्लिम लीग ने पिछड़ों को अलग सीट देने का समर्थन किया। वहीं 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा चुनी गई। तब मुस्लिम लीग के समर्थन से ही आंबेडकर बंगाल से चुनकर आए। 1947 में बंगाल के बंटवारे के बाद जब ये सीट नल एंड वॉयड हो गई। तब बॉम्बे से आंबेडकर को दोबारा चुना गया। इस बार कांग्रेस के समर्थन से।
बहरहाल धर्म के मसले पर वापिस आएं तो आंबेडकर का मुख्य उद्देश्य पिछड़ों को अधिकार दिलाना था। इस कोशिश में वह लगातार कार्यरत रहे। राजनीतिक शक्ति जुटाने के लिए उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत को ऑप्शन के रूप में देखा लेकिन अंत में चुना बौद्ध धर्म को।
बौद्ध धर्म ही क्यों?
जैसा शुरुआत में हमने बताया था आंबेडकर धर्म के सांसारिक महत्त्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व पर भी जोर देते हैं। एक कोट देखिए उनका, ‘बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य’ नामक लेख में वह लिखते हैं, 'व्यक्ति का जन्म समाज की सेवा के लिए नहीं, उसकी अपनी मुक्ति के लिए होता है।' दिलचस्प है न? एक व्यक्ति जिसे सामजिक सुधार की कुंजी माना जाता है। व्यक्ति की मुक्ति पर जोर दे रहा है। आंबेडकर के अनुसार व्यक्ति की आजादी और समाज सुधार एक ही सिरे के दो पहलू हैं। इसलिए उन्होंने कभी धर्म से अलग होने की बात नहीं कही। उनके हिसाब से व्यक्ति का विकास तीन चीजों से होता है- करुणा, समानता और स्वतंत्रता। ये तीन गुण किसी भी धर्म के लिए आवश्यक हैं लेकिन जाति प्रथा के चलते हिंदू धर्म इनसे विहीन था। वहीं इस्लाम में भी गैर मुस्लिम के समानता और स्वतंत्रता नदारद थी। समानता के पहलू पर वह पाते हैं कि तीनों ही धर्म स्वयं को विशेष घोषित करते हैं।
यह भी पढ़ें- दुकानदारों के गाल चीरने वाले अलाउद्दीन खिलजी के आखिरी दिनों की कहानी
आंबेडकर लिखते हैं, 'ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह ने की है जो खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं। जो इस बात को नहीं मानता, वह ईश्वर के दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। इस्लाम के संस्थापक मुहम्मद ना सिर्फ़ खुद को पैग़म्बर घोषित करते हैं, बल्कि जन्नत में जाने के लिए ये मानना भी ज़रूरी है कि वह आख़िरी पैग़म्बर हैं। उनके बाद और कोई पैग़म्बर नहीं पैदा हो सकता। हिंदू धर्म के बारे में आंबेडकर कहते हैं, हिंदू धर्म में कृष्ण ने ईसा मसीह और मुहम्मद से भी आगे जाकर खुद को ईश्वर घोषित कर दिया।' अंत में आंबेडकर इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हैं। बुद्ध एक साधारण इंसान थे। उन्होंने कभी भी ईश्वर होने का दावा नहीं किया। कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने खुद को मुक्ति देने वाला ना कहकर मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला कहा।
साइंटिफिक टेम्परामेंट पर भी आंबेडकर का बड़ा जोर था इसलिए धर्म के पारलौकिक यानी आत्मा परमात्मा की बात करने वाले पक्ष से उन्होंने किनारा किया। साथ ही लिखा कि धर्म में आस्था की जो शर्त है, वह फ़िजूल है। आंबेडकर लिखते हैं, 'हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म का आधार आस्था है। इन धर्मों में एक व्यक्ति ने जो कह दिया, वह पत्थर की लकीर था। उस पर ना सवाल उठाया जा सकता है, ना ही कोई तर्क किया जा सकता है।' इसके बरअक्स गौतम बुद्ध के बारे में आंबेडकर लिखते हैं, 'बुद्ध अंतिम सत्य का दावा नहीं करते। बुद्ध ने कहा अप्प दीपो भव। यानी खुद अपने दीपक बनो। स्वयं सत्य को जानो।'
बुद्ध पर आंबेडकर ने क्या लिखा?
‘महापरिनिर्वाण-सूत्र’ का रिफरेंस देते हुए आंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध की बात सिर्फ इसलिए सही नहीं है कि वह बुद्ध ने कही है। जो सत्य है, उसके लिए आस्था की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पानी सत्य है क्योंकि वह है, इसलिए नहीं कि आप उसमें आस्था रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आंबेडकर के सिख धर्म पर विचार को जानना जरूरी है। सिख धर्म में शिक्षाओं के हिसाब से जाति व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी ऊंच-नीच होती है। ऐसा ही भारतीय ईसाईयों के बीच था। आंबेडकर के अनुसार इसका बड़ा कारण ये था कि धर्म आसानी से बदलाव को तैयार नहीं होते इसलिए पुराना ढर्रा चलता रहता है।
आंबेडकर के अनुसार बौद्ध धर्म इस मामले में बेहतर था क्योंकि उस पर भूतकाल का बोझ नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं को काल और परिस्थितियों के हिसाब से ढाला जा सकता है। बुद्ध ने स्वयं इसकी इजाजत दी है। बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति को आंबेडकर उदाहरण मानते हैं।
वह लिखते हैं, 'हिंदुओं में शूद्र और स्त्रियां धर्म उपदेशक नहीं हो सकते जबकि बुद्ध ने शूद्रों को अपने बराबर बिठाया और संघ में स्त्रियों को भिक्षु बनने का अधिकार दिया।' बौद्ध धर्म और हिन्दू धर्म में कुछ चीजें कॉमन है। मसलन कर्म का सिद्धांत, जिसके बल पर ये तर्क दिया जाता है कि कर्म के चलते ही इंसान अगले जन्म में ऊंची या नीची जाति में पैदा होता है। तो फिर बौद्ध धर्म अलग कैसे?
आंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए कर्म के सिद्धांत को नए सिरे से परिभाषित किया। वह लिखते हैं, 'विज्ञान के अनुसार बच्चा, माता और पिता के गुण लेकर पैदा होता है जबकि हिंदू धर्म के अनुसार बच्चा पिछले जन्मों के कर्मों का फल साथ लेकर पैदा होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर दलितों के शोषण के लिए खुद उन्हें ही दोषी ठहरा दिया गया। यह कहकर कि ये उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। बुद्ध ने कर्म के इस सिद्धांत को कभी नहीं माना। बुद्ध ने जब आत्मा को ही नहीं माना तो आत्मा के पुनर्जन्म का बुद्ध धर्म में कोई स्थान हो ही नहीं सकता। बुद्ध का ‘कर्म’ तात्कालिक है। अभी इसी जीवन में है। उसके लिए अगले जन्म का इंतज़ार नहीं करना पड़ता।'
ये तमाम आर्गुमेंट्स आंबेडकर के भाषणों और लेखों में मिलते हैं और ये इंटरनल डायलॉग आंबेडकर के मन में लम्बे समय तक चला। इसीलिए 1935 में वे हिन्दू धर्म त्यागने की बात कहते हैं जबकि बौद्ध धर्म उन्होंने 20 साल बाद ग्रहण किया।
14 अक्टूबर 1956: नागपुर में डॉक्टर आंबेडकर ने 3 लाख पैंसठ हजार लोगों के साथ डॉक्टर आंबेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। साथ ही 22 प्रतिज्ञाएं भी लीं। जिनमें शामिल था कि वे हिन्दू देवी देवताओं को अवतार नहीं मानेंगे। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के दो महीने बाद ही आंबेडकर की मृत्यु हो गई लेकिन इस कृत्य ने भारत में दलित और बुद्ध समाज पर गहरा प्रभाव डाला। 1950 की जनगणना में भारत में बौद्धों की संख्या 1।5 लाख से कम थी। आंबेडकर के धर्म परिवर्तन के 10 साल बाद, यह संख्या बढ़कर 32 लाख से अधिक हो गई।
आंबेडकर का धर्म परिवर्तन, भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना है, जिसने लम्बी बहस को जन्म देना चाहिए था। आंबेडकर के धर्म परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य ही था कि तमाम धरम अपनी गलतियों को पहचान सकें लेकिन जैसा आंबेडकर ने लगभग भविष्यवाणी की थी। ऐसा हुआ नहीं। धर्म बदले नहीं, कट्टर धार्मिकता बरक़रार रखते हुए आंबेडकर को अडॉप्ट कर लिया गया जबकि आंबेडकर इसी दोहराव की आलोचना कर रहे थे।
और पढ़ें
Copyright ©️ TIF MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED | All Rights Reserved | Developed By TIF Technologies
CONTACT US | PRIVACY POLICY | TERMS OF USE | Sitemap




